भारतीय सिनेमा-निर्माण के शताब्दी वर्ष में आयोजित हमारे इस विशेष अनुष्ठान- ‘स्मृतियों के झरोखे से’ के एक नए अंक में आपका स्वागत है। विगत एक सौ वर्षों में भारतीय जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला और सर्वसुलभ कोई माध्यम रहा है तो वह है, सिनेमा। 3मई, 1913 को मूक सिनेमा से आरम्भ इस यात्रा का पहला पड़ाव 1931 में आया, जब हमारा सिनेमा सवाक हुआ। इस स्तम्भ में हम आपसे मूक और सवाक युग के कुछ विस्मृत ऐतिहासिक क्षणों को साझा कर रहे हैं।
‘राजा हरिश्चन्द्र’ से पहले
पिछले अंकों में हम आपसे यह चर्चा कर चुके हैं कि 3मई, 1913 को विदेशी उपकरणों की सहायता से किन्तु भारतीय कथानक पर भारतीय कलाकारों द्वारा पहले कथा-चलचित्र ‘राजा हरिश्चन्द्र’ का निर्माण और प्रदर्शन हुआ था। इस पहली मूक फिल्म का प्रदर्शन 1913 में हुआ था, किन्तु इस सुअवसर के लिए भारतीयों ने 1896 से ही प्रयास करना शुरू कर दिया था। पिछले अंक में हमने ऐसे ही कुछ प्रयासों की चर्चा की थी। आज ऐसे कुछ और प्रयासों की हम चर्चा करेंगे।
वर्ष 1900 में मुम्बई के एक विद्युत इंजीनियर एफ.बी. थानावाला ने एक वृत्तचित्र ‘स्प्लेंडिड न्यू व्यू आफ़ बाम्बे’ का निर्माण किया था। इस फिल्म का प्रदर्शन कुछ अन्य विदेशी फिल्म के साथ किया गया था। इस समय तक सिनेमा माध्यम का उपयोग किसी रोचक विषय के फिल्मांकन तक सीमित था। किसी निर्धारित कथानक पर फिल्म निर्माण की सोच का विकास नहीं हो सका था। कथाचित्र निर्माण का प्रयास सर्वप्रथम कलकत्ता के सेन बन्धुओं (हीरालाल और मोतीलाल) ने किया। सेन बन्धुओं ने 1898 में लंदन से एक ‘बाइस्कोप
 |
| हीरालाल सेन |
सेन बन्धुओं ने अपना यह प्रयास जारी रखा। 1903 में उन्होने बांग्ला के सुविख्यात रंगकर्मी अमरनाथ दत्त के सहयोग से कुछ ऐसे मंच-नाटकों का फिल्मांकन किया, जिनके कथानक जन-जन में लोकप्रिय थे। 6जून, 1903 को कलकत्ता के क्लासिक थियेटर में एक पूर्णकालिक बांग्ला नाटक के फिल्मांकन का सफल प्रदर्शन हुआ था। बांग्ला के चर्चित साहित्यकार बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय कृत सीताराम, अलीबाबा, भ्रमर, हरिराज, सरला और बुद्धदेव जैसे नाटकों का फिल्मांकन कर सेन बन्धुओं ने मूक फिल्मों की सफलता का एक नया द्वार खोला। सेन बन्धुओं को किसी उत्पाद के प्रचार के लिए पहली फिल्म बनाने का श्रेय भी दिया जाएगा। उन्होने 1903 में ही ‘जावाकुसुम केश तेल’ के प्रचार के लिए विज्ञापन-फिल्म का निर्माण भी किया था।
सवाक युग के धरोहर
 |
| विनायक राव पटवर्धन |
सवाक फिल्मों के आरम्भिक दौर में 1जनवरी, 1932 को एक बेहद सफल फिल्म ‘माधुरी’ का प्रदर्शन हुआ था। चौथी शताब्दी में गुप्तवंश शासन के एक ऐतिहासिक कथानक पर आधारित इस फिल्म में युद्ध के रोमांचक दृश्य थे। मोहनलाल इस फिल्म के पटकथा लेखक थे। मालवा और कन्नौज राज्यों के बीच की शत्रुता और उनके बीच हुए युद्ध का प्रसंग फिल्म का केन्द्रविन्दु था। एक ऐसे ही प्रसंग में नायिका माधुरी पुरुष वेष धारण कर कन्नौज के महासामन्त से युद्ध कर मालवा के राजकुमार को मुक्त कराती है। फिल्म के संगीतकार प्राणसुख नायक थे, जिन्होने तत्कालीन शास्त्रीय गायक विनायक राव पटवर्धन से कई मधुर गीत गवाए, जिसके बल पर फिल्म को आशातीत सफलता मिली। विनायक राव पटवर्धन फिल्म के नायक और सुलोचना नायिका थीं।
इसी फिल्म में विनायक राव के गाये गीत- ‘सरिता सुगन्ध शोभे बसन्त...’ का ग्रामोफोन रेकार्ड भी बना था। ग्रामोफोन कम्पनी ने पहली बार किसी भारतीय फिल्म के संगीत का रेकार्ड बनाया था। ‘धुनों की यात्रा’ पुस्तक के लेखक पंकज राग के अनुसार- ‘फिल्म संगीत का पहला रेकार्ड जारी होने का यह तथ्य अकेले ही प्राणसुख नायक को एक ऐतिहासिक महत्त्व दे जाता है’। 1932 में प्रदर्शित फिल्म ‘माधुरी’ के दो दुर्लभ गीत आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे है। पहला गीत- ‘अहंकार करके हमेशा...’ तीनताल में और दूसरा गीत- ‘परमुख वाली तू कमला...’ द्रुत एकताल में निबद्ध किया गया है। प्राणसुख नायक के संगीतबद्ध किये दोनों गीतों को विनायक राव पटवर्धन ने स्वर दिया है।
फिल्म माधुरी : ‘अहंकार करके हमेशा...’ विनायक राव पटवर्धन
फिल्म माधुरी : ‘परमुख वाली तू कमला...’ विनायक राव पटवर्धन
इसी गीत के साथ इस अंक से हम विराम लेते हैं। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी, अवश्य लिखिएगा। आपकी प्रतिक्रिया, सुझाव और समालोचना से हम इस स्तम्भ को और भी सुरुचिपूर्ण रूप प्रदान कर सकते हैं। ‘स्मृतियों के झरोखे से : भारतीय सिनेमा के सौ साल’ के आगामी अंक में बारी है- ‘मैंने देखी पहली फिल्म’ प्रतियोगिता की। हमारे अगले अंक में जो आलेख शामिल होगा वह प्रतियोगी वर्ग से होगा। आपके आलेख हमें जिस क्रम से प्राप्त हुए हैं, उनका प्रकाशन हम उसी क्रम से कर रहे हैं। यदि आपने ‘मैंने देखी पहली फिल्म’ प्रतियोगिता के लिए अभी तक अपना संस्मरण नहीं भेजा है तो हमें तत्काल radioplaybackindia@live.com पर मेल करें।
कृष्णमोहन मिश्र

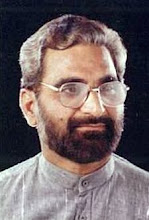

Comments
since i love to learn more and more.
Also visit my page; buy natox