स्वरगोष्ठी – 118 में आज
यूँ बनी पहली भोजपुरी फिल्म- ‘गंगा मैया तोहें पियरी चढ़इबो’
यूँ बनी पहली भोजपुरी फिल्म- ‘गंगा मैया तोहें पियरी चढ़इबो’
 संगीत-प्रेमियों की साप्ताहिक महफिल ‘स्वरगोष्ठी’ के एक नये अंक के साथ
मैं कृष्णमोहन मिश्र पुनः उपस्थित हूँ। भारतीय सिनेमा के इतिहास में 4
अप्रैल, 1963 की तिथि इसलिए बेहद महत्त्वपूर्ण है कि इस दिन पहली भोजपुरी
फिल्म ‘गंगा मैया तोहें पियरी चढ़इबो’ का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन वाराणसी
के प्रकाश सिनेमाघर में हुआ था। इस तिथि के अनुसार भोजपुरी सिनेमा प्रदर्शन
की आधी शताब्दी पूर्ण कर चुका है। इस अवसर पर हम इस फिल्म के निर्माण से
जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्यों और रोचक प्रसंगों की चर्चा इस विशेष अंक में कर
रहे हैं। आज का यह अंक प्रस्तुत कर रहे हैं, युवा फ़िल्म पत्रकार, शोधार्थी,
स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्री व लघु फिल्मकार तथा पटना स्थित सिने सोसाइटी के
मीडिया प्रबन्धक, रविराज पटेल।
संगीत-प्रेमियों की साप्ताहिक महफिल ‘स्वरगोष्ठी’ के एक नये अंक के साथ
मैं कृष्णमोहन मिश्र पुनः उपस्थित हूँ। भारतीय सिनेमा के इतिहास में 4
अप्रैल, 1963 की तिथि इसलिए बेहद महत्त्वपूर्ण है कि इस दिन पहली भोजपुरी
फिल्म ‘गंगा मैया तोहें पियरी चढ़इबो’ का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन वाराणसी
के प्रकाश सिनेमाघर में हुआ था। इस तिथि के अनुसार भोजपुरी सिनेमा प्रदर्शन
की आधी शताब्दी पूर्ण कर चुका है। इस अवसर पर हम इस फिल्म के निर्माण से
जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्यों और रोचक प्रसंगों की चर्चा इस विशेष अंक में कर
रहे हैं। आज का यह अंक प्रस्तुत कर रहे हैं, युवा फ़िल्म पत्रकार, शोधार्थी,
स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्री व लघु फिल्मकार तथा पटना स्थित सिने सोसाइटी के
मीडिया प्रबन्धक, रविराज पटेल।  |
| रविराज पटेल |
 |
| नजीर हुसैन |
 |
| फिल्म की नायिका कुमकुम |
हफ्ता-दस दिनों का समय लगा होगा, जिसमें लगभग कलाकारों का चयन एवं शूटिंग स्थल तय करने के बाद इस पर कुल बजट एक लाख पचास हज़ार रूपये तय किया गया। किन्तु फिल्म पूरी होने तक यह बजट पूर्वनिर्धारित से तीन गुना से भी अधिक यानि पाँच लाख रूपये तक पहुँच गया था। मुकम्मल तैयारी के पश्चात 16 फरवरी, 1962 को बिहार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा एवं उनकी धर्मपत्नी किशोरी सिन्हा जी की उपस्थिति में इस फिल्म का मुहूर्त पटना स्थित शहीद स्मारक परिसर में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर फिल्म की नायिका अभिनेत्री कुमकुम के साथ चरित्र अभिनेता नजीर हुसैन और नायक असीम कुमार के एक छोटे से दृश्य का फिल्मांकन हुआ। इसके बाद फिल्म की कुछेक आउटडोर शूटिंग मनेर (पटना) में हुई, जिसमें पंचायत, ताड़ीखाना (निरालय) तथा पालकी आदि दृश्यों को फिल्माया गया। वहीँ वाराणसी में गंगाघाट, कबीरचौरा, चौक आदि के अलावा गाजीपुर में भी फिल्म के कुछ महत्त्वपूर्ण दृश्यों को कैमरे में समेटा गया। आधिकांश शूटिंग बम्बई के प्रकाश तथा श्रीकान्त स्टूडियो में की गई।
 भोजपुरी की इस पहली फिल्म को बनने में कुल अवधि लगभग एक वर्ष लगी थी। पूरी तरह से तैयार फिल्म को निर्माता विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी ने 21 फरवरी, 1963 को तत्कालीन राष्ट्रपति देशरत्न डॉ. राजेन्द्रप्रसाद को पटना के सदाकत आश्रम में समर्पित किया। यानि 21 फरवरी, 1963 को इस फ़िल्म का उद्घाटन समारोह समझा गया। इसके एक दिन बाद अर्थात 22 फरवरी, 1963 को फिल्म का एक प्रीमियर शो पटना के वीणा सिनेमा में रखा गया। लेकिन इसके व्यावसायिक प्रदर्शन की शुरुआत 4 अप्रैल, 1963 को वाराणसी के प्रकाश टॉकीज (अब बन्द हो चुका है) से हुई। 21 फरवरी से 4 अप्रैल के बीच एकतालीस दिनों की अवधि का अन्तर इसलिए आया कि उन्हीं दिनों डॉ. राजेन्द्र बाबू अस्वस्थ हो गए थे। अस्वस्थता की स्थिति में ही उन्होने 25 फरवरी, 1963 को इस फिल्म के निर्माण पर पूरे दल को बधाई-पत्र भेजा था। इसी दौरान उन्होने बीमार रहते हुए भी 1 मार्च, 1963 को फिल्म के तमाम कलाकारों से मिलने का कार्यक्रम तय किया था। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था, इस निर्धारित तिथि के ठीक एक दिन पूर्व यानि 28 फरवरी, 1963 को ही उनकी ह्रदयगति रुक गई और वे अमरत्व को प्राप्त कर गए।
भोजपुरी की इस पहली फिल्म को बनने में कुल अवधि लगभग एक वर्ष लगी थी। पूरी तरह से तैयार फिल्म को निर्माता विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी ने 21 फरवरी, 1963 को तत्कालीन राष्ट्रपति देशरत्न डॉ. राजेन्द्रप्रसाद को पटना के सदाकत आश्रम में समर्पित किया। यानि 21 फरवरी, 1963 को इस फ़िल्म का उद्घाटन समारोह समझा गया। इसके एक दिन बाद अर्थात 22 फरवरी, 1963 को फिल्म का एक प्रीमियर शो पटना के वीणा सिनेमा में रखा गया। लेकिन इसके व्यावसायिक प्रदर्शन की शुरुआत 4 अप्रैल, 1963 को वाराणसी के प्रकाश टॉकीज (अब बन्द हो चुका है) से हुई। 21 फरवरी से 4 अप्रैल के बीच एकतालीस दिनों की अवधि का अन्तर इसलिए आया कि उन्हीं दिनों डॉ. राजेन्द्र बाबू अस्वस्थ हो गए थे। अस्वस्थता की स्थिति में ही उन्होने 25 फरवरी, 1963 को इस फिल्म के निर्माण पर पूरे दल को बधाई-पत्र भेजा था। इसी दौरान उन्होने बीमार रहते हुए भी 1 मार्च, 1963 को फिल्म के तमाम कलाकारों से मिलने का कार्यक्रम तय किया था। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था, इस निर्धारित तिथि के ठीक एक दिन पूर्व यानि 28 फरवरी, 1963 को ही उनकी ह्रदयगति रुक गई और वे अमरत्व को प्राप्त कर गए।
पहली भोजपुरी फिल्म की व्यावसायिक शुरुआत देवभूमि वाराणसी से हुई और इसकी गूँज विश्व भर में गुंजायमान हुई। कुमकुम की करुणा, असीम का अभिनय, नजीर के मुरीद कौन नहीं हुए? वहीँ, इस फिल्म में शैलेंद्र के गीत और चित्रगुप्त के संगीत ने भी लोगों को कभी भावविह्वल किया तो कभी खूब खिलखिलाया। प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि वाराणसी के प्रकाश टॉकीज में तो रात-दिन मेले जैसा दृश्य बना रहता था। लोग दूर-दराज से खाना, बिछावन के साथ एक दिन पूर्व ही टॉकीज परिसर में डेरा जमा देते थे। उस समय एक नई कहावत भी चल पड़ी थी- “गंगा नहा, बाबा बिसनाथ दरसन करा, गंगा मैया... देखा, तब घरे जा...”। इसकी सन्देशात्मक लोकप्रियता एवं आकर्षण का ही प्रतिफल कहें कि तत्कालीन केन्द्रीय विदेश एवं गृहमंत्री लालबहादुर शास्त्री जी (बाद में देश के द्वितीय प्रधानमंत्री बने), केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्यमंत्री सत्यनारायण सिन्हा जी एवं परिवहनमंत्री जगजीवन राम जी जैसी विभूति ने भी इसे देखने की इच्छा जाहिर की थी। फलतः 11 अक्टूबर, 1963 को दिल्ली के गोलचा सिनेमा में फिल्म के विशेष प्रदर्शन का आयोजन किया गया। फिल्म की कहानी इतनी प्रभावकारी और ह्रदय विदारक थी कि प्रदर्शन के दौरान शास्त्री जी की आँखे नम हो गईं थी। भोजपुरी भाषा में बनी यह पहली फिल्म “गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो” ने किसी भी अन्य भाषाओँ के मुकाबले में कम सफलता एवं लोकप्रियता हासिल नहीं की थी, बल्कि समाज में दहेज, बेमेल विवाह, विधवा विवाह, सामन्ती विचारों, सूदखोरी, अशिक्षा, सामाजिक जिम्मेदारी तथा अन्धविश्वास परम्पराओं से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं का एक सही और संवेदनशील चित्र उपस्थित हुआ।
अब हम आपको इस फिल्म का सर्वाधिक लोकप्रिय शीर्षक गीत सुनवाते हैं। इसके गीतकार शैलेन्द्र और संगीतकार चित्रगुप्त थे।
फिल्म गंगा मैया तोहें पियरी चढ़इबो : ‘हे गंगा मैया तोहें...’ : लता और उषा मंगेशकर
आज की पहेली
‘स्वरगोष्ठी’ के 118वें अंक की पहेली में आज हम आपको एक रागमाला गीत का अंश सुनवा रहे है। इसे सुन कर आपको दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रतिभागियों से अनुरोध है कि पहेली में गीत/संगीत का जो अंश आपको सुनवाया जा रहा है, राग की पहचान केवल उतने ही अंश से करें। रागमाला के अन्य रागों का अपने उत्तर में उल्लेख न करें। पहेली के 120वें अंक तक जिस प्रतिभागी के सर्वाधिक अंक होंगे, उन्हें इस श्रृंखला (सेगमेंट) का विजेता घोषित किया जाएगा।
1 – गीत के इस अंश को सुन कर पहचानिए कि यह अंश किस राग पर आधारित है?
2 – यह गीतांश किस ताल में निबद्ध किया गया है?
आप अपने उत्तर केवल swargoshthi@gmail.com पर ही शनिवार मध्यरात्रि तक भेजें। comments में दिये गए उत्तर मान्य नहीं होंगे। विजेता का नाम हम ‘स्वरगोष्ठी’ के 120वें अंक में प्रकाशित करेंगे। इस अंक में प्रस्तुत गीत-संगीत, राग, अथवा कलासाधक के बारे में यदि आप कोई जानकारी या अपने किसी अनुभव को हम सबके बीच बाँटना चाहते हैं तो हम आपका इस संगोष्ठी में स्वागत करते हैं। आप पृष्ठ के नीचे दिये गए comments के माध्यम से या swargoshthi@gmail.com अथवा radioplaybackindia@live.com पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं।
पिछली पहेली के विजेता
‘स्वरगोष्ठी’ के 116वें अंक में हमने आपको 1953 में प्रदर्शित फिल्म ‘हमदर्द’ से लिये गए रागमाला गीत का एक अंश सुनवा कर आपसे दो प्रश्न पूछे थे। पहले प्रश्न का सही उत्तर है- राग जोगिया और दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है- तीनताल। दोनों प्रश्नो के सही उत्तर बैंगलुरु के पंकज मुकेश, लखनऊ के प्रकाश गोविन्द और जबलपुर से क्षिति तिवारी ने दिया है। तीनों प्रतिभागियों को ‘रेडियो प्लेबैक इण्डिया’ की ओर से हार्दिक बधाई।
झरोखा अगले अंक का
मित्रों, ‘रेडियो प्लेबैक इण्डिया’ के साप्ताहिक स्तम्भ ‘स्वरगोष्ठी’ पर
लघु श्रृंखला ‘रागों के रंग रागमाला गीत के संग’ अगले अंक से पुनः जारी
होगा। अगले अंक का रागमाला गीत तीन अलग-अलग राग पर आधारित अन्तरॉ वाला गीत
है। अगले अंक में हम इसी रागमाला गीत पर चर्चा करेंगे। आप भी हमारे आगामी
अंकों के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़े नये विषयों, रागों और अपनी
प्रिय रचनाओं की फरमाइश कर सकते हैं। हम आपके सुझावों और फरमाइशों को पूरा
सम्मान देंगे। अगले अंक में रविवार को प्रातः 9-30 ‘स्वरगोष्ठी’ के इस मंच
पर आप सभी संगीत-रसिकों की हमें प्रतीक्षा रहेगी।
शोध एवं आलेख : रविराज पटेल
प्रस्तुति : कृष्णमोहन मिश्र

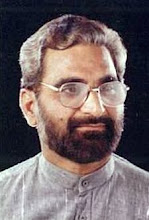
Comments