स्वरगोष्ठी – 346 में आज
फिल्मी गीतों में ठुमरी के तत्व – 3 : गायिका राजकुमारी के स्वर
राग पीलू में नायक को रोकने के लिए नायिका की कोशिश – “चले जइयो बेदर्दा मैं रोय मरूँगी...”
 | |
| गायिका राजकुमारी |
फिल्मी
ठुमरियों की इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में आपने राधा-कृष्ण की होली का
कल्पनाशील चित्रण महसूस किया था; किन्तु आज के ठुमरी गीत में नायिका अपने
प्रियतम से बिछड़ना ही नहीं चाहती। उसे रोकने के लिए नायिका तरह-तरह के
प्रयत्न करती है, तर्क देती है, यहाँ तक कि वह अपने प्रियतम को धमकी भी
देती है। पिछली कड़ी में हम यह भी चर्चा कर चुके हैं कि ठुमरी शैली में रस,
रंग और भाव की प्रधानता होती है। ख़याल शैली के द्रुत लय की रचना (छोटा
ख़याल) और ठुमरी में मूलभूत अन्तर यही होता है कि छोटा ख़याल में शब्दों की
अपेक्षा राग के स्वरों और स्वर संगतियों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है,
जबकि ठुमरी में रस के अनुकूल भावाभिव्यक्ति पर ध्यान रखना पड़ता है। प्रायः
ठुमरी गायक / गायिका को एक ही शब्द अथवा शब्द समूह को अलग-अलग भाव में
प्रस्तुत करना होता है। इस प्रक्रिया में राग के निर्धारित स्वरों में
कहीं-कहीं परिवर्तन करना पड़ता है।
ठुमरी की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत-मतान्तर हैं। सामान्य धारणा है कि 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में ठुमरी का जन्म हुआ। परन्तु यह धारणा पूरी तरह ठीक नहीं है। 19वीं शताब्दी से काफी पहले भारतीय संगीत शास्त्र इतना समृद्ध था कि उसमें किसी नई शैली के जन्म लेने की सम्भावना नहीं थी। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में गीत के मूल तत्वों का जो निरूपण किया गया है, उसके अन्तर्गत सभी प्रकार के गीत किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। दरअसल नवाब वाजिद अली शाह संगीत, नृत्य प्रेमी थे और संरक्षक भी। उन्नीसवीं शताब्दी में ही नवाब वाजिद अली शाह और कदरपिया नामक संगीतज्ञ ने कथक नृत्य के साथ गायन के लिए कई प्रयोग किये। द्रुत लय के ख़याल, अवध क्षेत्र की प्रचलित लोक संगीत शैलियों तथा ब्रज क्षेत्र की कृष्णलीला से सम्बन्धित गेय पदों का नृत्य के साथ प्रयोग किया गया। नवाब के दरबारी गायक उस्ताद सादिक अली खाँ का योगदान भी इन प्रयोगों में था। नवाब वाजिद अली शाह ने खुद "अख्तरपिया" उपनाम से इस प्रकार के कई गीत रचे। नवाबी शासनकाल तक नृत्य के लिए तैयार की गईं ऐसी रचनाओं को "नाट्यगीति" या "काव्यगीति" ही कहा जाता था। इस शैली का "ठुमरी" नामकरण 1856 के आसपास प्रचलित हुआ। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से "ठुमरी" की उत्पत्ति हुई; यह कहना उपयुक्त न होगा। हाँ; नवाब के दरबार में यह एक शैली के रूप में विकसित हुई और यहीं पर "ठुमरी" के रूप में इस शैली की पहचान बनी।
ठुमरी की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत-मतान्तर हैं। सामान्य धारणा है कि 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में ठुमरी का जन्म हुआ। परन्तु यह धारणा पूरी तरह ठीक नहीं है। 19वीं शताब्दी से काफी पहले भारतीय संगीत शास्त्र इतना समृद्ध था कि उसमें किसी नई शैली के जन्म लेने की सम्भावना नहीं थी। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में गीत के मूल तत्वों का जो निरूपण किया गया है, उसके अन्तर्गत सभी प्रकार के गीत किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। दरअसल नवाब वाजिद अली शाह संगीत, नृत्य प्रेमी थे और संरक्षक भी। उन्नीसवीं शताब्दी में ही नवाब वाजिद अली शाह और कदरपिया नामक संगीतज्ञ ने कथक नृत्य के साथ गायन के लिए कई प्रयोग किये। द्रुत लय के ख़याल, अवध क्षेत्र की प्रचलित लोक संगीत शैलियों तथा ब्रज क्षेत्र की कृष्णलीला से सम्बन्धित गेय पदों का नृत्य के साथ प्रयोग किया गया। नवाब के दरबारी गायक उस्ताद सादिक अली खाँ का योगदान भी इन प्रयोगों में था। नवाब वाजिद अली शाह ने खुद "अख्तरपिया" उपनाम से इस प्रकार के कई गीत रचे। नवाबी शासनकाल तक नृत्य के लिए तैयार की गईं ऐसी रचनाओं को "नाट्यगीति" या "काव्यगीति" ही कहा जाता था। इस शैली का "ठुमरी" नामकरण 1856 के आसपास प्रचलित हुआ। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से "ठुमरी" की उत्पत्ति हुई; यह कहना उपयुक्त न होगा। हाँ; नवाब के दरबार में यह एक शैली के रूप में विकसित हुई और यहीं पर "ठुमरी" के रूप में इस शैली की पहचान बनी।
"ठुमरी"
का विकास-क्रम कथक नृत्य में भाव प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको जो
ठुमरी गीत सुनाने जा रहे हैं, वह भी नृत्य पर फिल्माया गया है। 1949 में
निर्मित फिल्म "बेक़सूर" में गायिका राजकुमारी द्वारा गायी राग "पीलू" में
निबद्ध इस ठुमरी को शामिल किया गया था। राग पीलू काफी थाट का अत्यन्त
लोकप्रिय राग है। इस राग के आरोह में ऋषभ और धैवत वर्जित होता है और अवरोह
में सभी सात स्वर प्रयोग किये जाते हैं। राग का वादी स्वर गान्धार और
संवादी स्वर निषाद है। ऋषभ, गान्धार, धैवत और निषाद स्वरों का दोनों रूप
प्रयोग किया जाता है। इस राग को गाने-बजाने के समय प्रायः अनेक रागों की
छाया दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसे संकीर्ण जाति का राग कहा जाता है। यह चंचल
और श्रृंगार प्रकृति का राग है, अतः इस राग में ठुमरी, टप्पा, भजन और
फिल्मी गीत अधिक प्रचलित हैं। आज हम आपको जो ठुमरी गीत सुनवाने जा रहे हैं,
वह एक पारम्परिक ठुमरी है, किन्तु फिल्म के गीतकार आरज़ू लखनवी ने आरम्भ
में और अन्तरों के मध्य विषय के अनुकूल उर्दू के शे'र भी जोड़े हैं। पूरब
अंग की ठुमरियों में, विशेष रूप से दादरा में ऐसे प्रयोग प्रारम्भ से ही
होते रहे हैं। फिल्मों में जब पारम्परिक गीत शामिल किये जाते है तब प्रायः
भ्रम की स्थिति बन जाती है। फ़िल्मी ठुमरियों के मामले में यह भ्रम कुछ
अधिक ही रहता है। रिकार्ड पर फिल्म के गीतकार का नाम अंकित होता ही है,
किन्तु ठुमरी की रचना में गीतकार की भूमिका तय करना कठिन होता है। साहिर
लुधियानवी और शैलेन्द्र ऐसे गीतकार हुए हैं, जिन्होंने परम्परागत शास्त्रीय
और उपशास्त्रीय रचनाओं से प्रेरणा लेकर फिल्मों में कई सफल गीतों की
रचनाएँ की हैं। कुछ गीतकारों ने परम्परागत ठुमरी के स्थायी को बरक़रार रखा,
किन्तु अन्तरा की पंक्तियाँ अपनी ओर से जोड़ दीं। इसी प्रकार संगीतकारों
की भूमिका भी अलग-अलग रही। इस ठुमरी गीत के संगीतकार अनिल विश्वास ने ठुमरी
के अनुकूल वाद्यों का बड़ा प्रभावी उपयोग किया है। अपने समय की सुप्रसिद्ध
गायिका राजकुमारी के स्वर में आप राग पीलू की इस ठुमरी का रसास्वादन
कीजिए।
पीलू ठुमरी : “चले जइयो बेदर्दा मैं रोय मरूँगी...” : राज कुमारी : फिल्म – बेकसूर
संगीत पहेली
‘स्वरगोष्ठी’
के 346वें अंक की संगीत पहेली में आज हम आपको 1953 में प्रदर्शित एक फिल्म
से एक ठुमरी गीत का एक अंश सुनवा रहे हैं। गीत के इस अंश को सुन कर आपको
निम्नलिखित तीन में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यदि आपको
तीन में से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर ज्ञात हो तो भी आप प्रतियोगिता में
भाग ले सकते हैं। इस वर्ष के अन्तिम अंक की ‘स्वरगोष्ठी’ तक जिस प्रतिभागी
के सर्वाधिक अंक होंगे, उन्हें इस वर्ष के पाँचवें सत्र का विजेता घोषित
किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे वर्ष के प्राप्तांकों की गणना के बाद
महाविजेताओं की घोषणा की जाएगी।
1 – इस गीतांश को सुन कर बताइए कि इसमें किस राग का स्पर्श है?
2 – इस गीत में प्रयोग किये गए ताल का नाम बताइए।
3 – इस गीत में किस सुप्रसिद्ध पार्श्वगायिका की आवाज़ है?
आप उपरोक्त तीन मे से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर केवल swargoshthi@gmail.com या radioplaybackindia@live.com पर ही शनिवार, 9 दिसम्बर, 2017 की मध्यरात्रि से पूर्व तक भेजें। आपको यदि उपरोक्त तीन में से केवल एक प्रश्न का सही उत्तर ज्ञात हो तो भी आप पहेली प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। COMMENTS
में दिये गए उत्तर मान्य हो सकते हैं, किन्तु उसका प्रकाशन पहेली का उत्तर
देने की अन्तिम तिथि के बाद किया जाएगा। विजेता का नाम हम उनके शहर,
प्रदेश और देश के नाम के साथ ‘स्वरगोष्ठी’ के 348वें अंक में
प्रकाशित करेंगे। इस अंक में प्रस्तुत गीत-संगीत, राग, अथवा कलासाधक के
बारे में यदि आप कोई जानकारी या अपने किसी अनुभव को हम सबके बीच बाँटना
चाहते हैं तो हम आपका इस संगोष्ठी में स्वागत करते हैं। आप पृष्ठ के नीचे
दिये गए COMMENTS के माध्यम से तथा swargoshthi@gmail.com अथवा radioplaybackindia@live.com पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं।
पिछली पहेली के विजेता
‘स्वरगोष्ठी’
की 344वीं कड़ी की पहेली में हमने आपको 1947 में प्रदर्शित फिल्म “आपकी
सेवा में” से एक ठुमरीनुमा गीत का अंश सुनवा कर आपसे तीन में से किन्हीं दो
प्रश्नों का उत्तर पूछा था। पहले प्रश्न का सही उत्तर है, राग - पीलू, दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है, ताल – सोलह मात्रा का जत ताल और तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है, स्वर – लता मंगेशकर।
इस अंक की पहेली प्रतियोगिता में प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले हमारे प्रतिभागी हैं – चेरीहिल न्यूजर्सी से प्रफुल्ल पटेल, जबलपुर, मध्यप्रदेश से क्षिति तिवारी, पेंसिलवेनिया, अमेरिका से विजया राजकोटिया, वोरहीज, न्यूजर्सी से डॉ. किरीट छाया और हैदराबाद से डी. हरिणा माधवी।
आशा है कि हमारे अन्य पाठक / श्रोता भी नियमित रूप से साप्ताहिक स्तम्भ
‘स्वरगोष्ठी’ का अवलोकन करते रहेंगे और पहेली प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
उपरोक्त सभी प्रतिभागियों को ‘रेडियो प्लेबैक इण्डिया’ की ओर से हार्दिक
बधाई।
अपनी बात
मित्रों,
‘रेडियो प्लेबैक इण्डिया’ के साप्ताहिक स्तम्भ ‘स्वरगोष्ठी’ पर जारी हमारी
नई श्रृंखला “फिल्मी गीतों में ठुमरी के तत्व” की आज की कड़ी में आपने 1949
में निर्मित और 1950 में प्रदर्शित फिल्म “बेकसूर” के ठुमरी गीत का
रसास्वादन किया। इस श्रृंखला में हम आपसे कुछ ऐसे फिल्मी गीतों पर चर्चा
करेंगे जिसमें आपको ठुमरी शैली के दर्शन होंगे। आज आपने जो गीत सुना, उसमें
राग पीलू का स्पर्श है। इस श्रृंखला में भी हम आपसे फिल्मी ठुमरियों पर
चर्चा कर रहे हैं और शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत और रागों पर चर्चा भी
करेंगे। हमारी वर्तमान और आगामी श्रृंखलाओं के लिए विषय, राग, रचना और
कलाकार के बारे में यदि आपकी कोई फरमाइश हो तो हमें swargoshthi@gmail.com पर अवश्य लिखिए। अगले अंक में रविवार को प्रातः 7 बजे हम ‘स्वरगोष्ठी’ के इसी मंच पर सभी संगीत-प्रेमियों का स्वागत करेंगे।
प्रस्तुति : कृष्णमोहन मिश्र

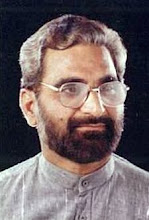
Comments