भूली-बिसरी यादें
भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष में आयोजित विशेष श्रृंखला ‘स्मृतियों के
झरोखे से’ के एक नये अंक के साथ मैं कृष्णमोहन मिश्र अपने साथी सुजॉय
चटर्जी के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ और आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज
मास का तीसरा गुरुवार है और इस दिन हम आपके लिए मूक और सवाक फिल्मों की कुछ
रोचक दास्तान लेकर आते हैं। तो आइए पलटते हैं, भारतीय फिल्म-इतिहास के कुछ
सुनहरे पृष्ठों को।
यादें मूक फिल्म-युग की : लन्दन में भी प्रदर्शित हुआ ‘राजा हरिश्चन्द्र’
दादा
साहब फालके की बनाई पहली भारतीय मूक फिल्म ‘राजा हरिश्चन्द्र’ से ही
भारतीय सिनेमा का इतिहास आरम्भ होता है। इस फिल्म का पूर्वावलोकन 21अप्रैल
1913 को और नियमित प्रदर्शन 3मई, 1913 को हुआ था। भारतीय दर्शकों के लिए
परदे पर चलती-फिरती तस्वीरें देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। दादा साहब
फालके ने इस फिल्म के निर्माण के लिए ‘फालके ऐंड कम्पनी’ की स्थापना बम्बई
(अब मुम्बई) में की थी। फिल्म ‘राजा हरिश्चन्द्र’ के प्रदर्शन के बाद फालके
ने अपनी अगली फिल्मों का निर्माण नासिक में किया। इसके लिए उन्होने अपना
कार्यालय और स्टूडिओ बम्बई से नासिक स्थानान्तरित किया।
 |
| प्रथम अभनेत्री कमला बाई |
वर्ष 1913
में ही दादा साहब फालके ने नासिक के स्टूडिओ में अपनी दूसरी फिल्म
‘भष्मासुर मोहिनी’ का निर्माण किया। 3245 फुट लम्बी यह फिल्म एक पौराणिक
कथानक पर आधारित थी। यह वही फिल्म थी, जिसमे भारतीय फिल्मों के इतिहास में
पहली बार स्त्री भूमिका में एक अभिनेत्री को प्रस्तुत किया गया था। पिछले
अंक में हम भारतीय सिनेमा के इतिहास की पहली अभिनेत्री कमला बाई की चर्चा
कर चुके हैं। फाल्के द्वारा निर्मित दूसरी फिल्म ‘भष्मासुर मोहिनी’ का
प्रदर्शन 27दिसम्बर, 1913 को हुआ था। इसी वर्ष एक ऐसी घटना भी हुई, जिससे
भारतीय सिनेमा को दक्षिण भारत में भी स्थायित्व मिला। रघुपति वेंकैया नायडू
उन दिनों घुमन्तू (टूरिंग) सिनेमा का व्यावसायिक प्रदर्शन दक्षिण भारत में
किया करते थे। ‘राजा हरिश्चन्द्र’ के सफल प्रदर्शन से उत्साहित होकर
उन्होने तत्कालीन मद्रास शहर में पहला स्थायी सिनेमाघर बनवाया। अगले वर्ष
अर्थात 1914 में जे.एफ. मदान ने दिल्ली में एक स्थायी सिनेमाघर- ‘एल्फ़िस्टन
पिक्चर पैलेस’ का निर्माण कराया था। दादा साहब फालके ने वर्ष 1913 में दो
मूक फिल्मों का निर्माण कर अपना जो वर्चस्व कायम किया था, वह अगले वर्ष
1914 में भी बना रहा। इस वर्ष फाल्के की तीसरी फिल्म ‘सावित्री-सत्यवान’ का
निर्माण और प्रदर्शन हुआ था। 6जून, 1914 को प्रदर्शित यह फिल्म भी एक
पौराणिक कथा पर आधारित थी। वर्ष 1914 की एक महत्त्वपूर्ण घटना यह भी थी कि
फिल्म ‘राजा हरिश्चन्द्र’ का प्रदर्शन लन्दन में हुआ था।
सवाक युग के धरोहर : पार्श्वगायन परम्परा का सूत्रपात फिल्म ‘धूप छाँव’ से हुआ
 भारतीय
फिल्मों में आवाज़ का आगमन 1931 में बनी फिल्म ‘आलमआरा’ से हुआ था। इस दौर
की फिल्मों में अभिनेता-अभिनेत्रियों को अपने गाने स्वयं गाने पड़ते थे।
वर्ष 1935 को हिन्दी सिने-संगीत के इतिहास का एक स्मरणीय वर्ष माना जाएगा।
संगीतकार रायचन्द्र बोराल ने, अपने सहायक और संगीतकार पंकज मल्लिक के साथ
मिलकर ‘न्यू थिएटर्स’ में प्लेबैक पद्धति, अर्थात पार्श्वगायन की शुरुआत
की। पर्दे के बाहर रेकॉर्ड कर बाद में पर्दे पर फ़िल्माया गया पहला गीत था
फ़िल्म ‘धूप छाँव’ का। इस फिल्म में के.सी. डे का गाया “तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफ़िर जाग ज़रा...” और “मन की आँखें खोल बाबा...”
लोकप्रिय गीतों में था। इन गीतों से पार्श्वगायन की शुरुआत ज़रूर हुई, पर
सही मायने में इन्हें प्लेबैक गीत नहीं कहा जा सकता क्योंकि के.सी. डे के
गाये इन गीतों को उन्हीं पर फ़िल्माया गया था। इन गीतों को सुन कर साफ़ महसूस
होता है कि इससे पहले के गीतों से इन प्री-रेकॉर्डेड गीतों के स्तर में
कितना अन्तर है। इस फ़िल्म में सहगल का गाया “अंधे की लाठी तू ही है...” और उमा शशि का गाया “प्रेम कहानी सखी सुनत सुहाये चोर चुराये माल...” तथा पहाड़ी सान्याल व उमा शशि का गाया युगल गीत “मोरी प्रेम की नैया चली जल में...”
भी फ़िल्म के चर्चित गाने थे। फिल्म इतिहासकार विजय कुमार बालकृष्णन के
अनुसार फिल्म ‘धूप छाँव’ में पहला प्रीरिकार्ड किया गीत, जो फिल्माया गया
था, वह के.सी. डे, सुप्रभा सरकार और साथियों का गाया गीत “मेरो घर मोहन आयो...” था। आइए, सुनते हैं इस पहले पार्श्वगायन के रूप में फिल्माए गीत को।
भारतीय
फिल्मों में आवाज़ का आगमन 1931 में बनी फिल्म ‘आलमआरा’ से हुआ था। इस दौर
की फिल्मों में अभिनेता-अभिनेत्रियों को अपने गाने स्वयं गाने पड़ते थे।
वर्ष 1935 को हिन्दी सिने-संगीत के इतिहास का एक स्मरणीय वर्ष माना जाएगा।
संगीतकार रायचन्द्र बोराल ने, अपने सहायक और संगीतकार पंकज मल्लिक के साथ
मिलकर ‘न्यू थिएटर्स’ में प्लेबैक पद्धति, अर्थात पार्श्वगायन की शुरुआत
की। पर्दे के बाहर रेकॉर्ड कर बाद में पर्दे पर फ़िल्माया गया पहला गीत था
फ़िल्म ‘धूप छाँव’ का। इस फिल्म में के.सी. डे का गाया “तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफ़िर जाग ज़रा...” और “मन की आँखें खोल बाबा...”
लोकप्रिय गीतों में था। इन गीतों से पार्श्वगायन की शुरुआत ज़रूर हुई, पर
सही मायने में इन्हें प्लेबैक गीत नहीं कहा जा सकता क्योंकि के.सी. डे के
गाये इन गीतों को उन्हीं पर फ़िल्माया गया था। इन गीतों को सुन कर साफ़ महसूस
होता है कि इससे पहले के गीतों से इन प्री-रेकॉर्डेड गीतों के स्तर में
कितना अन्तर है। इस फ़िल्म में सहगल का गाया “अंधे की लाठी तू ही है...” और उमा शशि का गाया “प्रेम कहानी सखी सुनत सुहाये चोर चुराये माल...” तथा पहाड़ी सान्याल व उमा शशि का गाया युगल गीत “मोरी प्रेम की नैया चली जल में...”
भी फ़िल्म के चर्चित गाने थे। फिल्म इतिहासकार विजय कुमार बालकृष्णन के
अनुसार फिल्म ‘धूप छाँव’ में पहला प्रीरिकार्ड किया गीत, जो फिल्माया गया
था, वह के.सी. डे, सुप्रभा सरकार और साथियों का गाया गीत “मेरो घर मोहन आयो...” था। आइए, सुनते हैं इस पहले पार्श्वगायन के रूप में फिल्माए गीत को।
फिल्म धूप छाँव : “मेरो घर मोहन आयो...” : के.सी. डे, सुप्रभा सरकार और साथी
 |
| पंकज मल्लिक |
फ़िल्म
‘धूप छाँव’ के गीतकार थे पण्डित सुदर्शन। प्लेबैक तकनीक के आने के बाद भी
कई वर्षों तक बहुत से अभिनेता स्वयं गीत गाते रहे, फिर धीरे धीरे अभिनेता
और गायक की अलग-अलग श्रेणी बन गई। ‘धूप छाँव’ में ही पारुल घोष, सुप्रभा
सरकार और हरिमति का गाया एक गीत था “मैं ख़ुश होना चाहूँ, हो न पाऊँ...”, जो
सही अर्थ में पहला प्लेबैक गीत था। इस तरह से इन तीन गायिकाओं को
फ़िल्म-संगीत की प्रथम पार्श्वगायिकाएँ होने का गौरव प्राप्त है। हरमन्दिर
सिंह ‘हमराज़’ को दिए एक साक्षात्कार में सुप्रभा सरकार ने पार्श्वगायन की
शुरुआत से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया था – “उन्होंने
(सुप्रभा सरकार ने) बताया कि फ़िल्मों में उनका प्रवेश 13 वर्ष की आयु में
तत्कालीन अभिनेत्री लीला देसाई के भाई के प्रयत्नों से हुआ था। सन् 1935
में जब ‘न्यू थिएटर्स’ द्वारा ‘जीवन मरण’ (बांग्ला) तथा ‘दुश्मन’ (हिन्दी)
का निर्माण शुरु हुआ तब पार्श्वगायन पद्धति का प्रथम उपयोग इसी फ़िल्म में
किया जाना था परन्तु फ़िल्म की शूटिंग के समय एक दृश्य में पेड़ से नीचे
कूदते समय नायिका लीला देसाई की टाँग टूट गई और फ़िल्म का निर्माण रुक गया।
इसी बीच फ़िल्म ‘धूप छाँव’ का निर्माण शुरु हुआ। निर्देशक नितिन बोस ने पहले
तो सुप्रभा सरकार की आवाज़ को नामंज़ूर ही कर दिया था, लेकिन एक समूह गीत
में सुप्रभा, हरिमती और पारुल घोष की आवाज़ों में रेकॉर्ड किया गया जो कि
बाद में प्रथम पार्श्वगीत के रूप में जाना गया।” उधर पंकज मल्लिक ने भी
अपनी आत्मकथा में पार्श्वगायन की शुरुआत का दिलचस्प वर्णन किया है। पंकज
राग लिखित किताब ‘धुनों की यात्रा’ से प्राप्त जानकारी के अनुसार– “नितिन
बोस स्टुडिओ जाते समय अपनी कार से पंकज मल्लिक के घर से उन्हें लेते हुए
जाते थे। एक दिन उनके घर के सामने कई बार हार्न देने पर भी पंकज मल्लिक
नहीं मिकले, और काफ़ी देर बाद अपने पिता के बताने पर कि नितिन बोस उनकी बाहर
कार में प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे हड़बड़ाते हुए बाहर आए और देरी का कारण
बताते हुए कहा कि वे अपने मनपसंद अंग्रेज़ी गानों का रेकॉर्ड सुनते हुए गा
रहे थे, इसी कारण हार्न की आवाज़ नहीं सुन सके। इसी बात पर नितिन बोस को
विचार आया कि क्यों न इसी प्रकार पार्श्वगायन लाया जाए। उन्होंने बोराल से
चर्चा की और अपने पूरे कौशल के साथ बोराल ने इस विचार को साकार करते हुए
इसे ‘धूप छाँव’ में आज़माया।” इस प्रकार भारतीय फिल्मों में पार्श्वगायन की
शुरुआत हुई। फिल्म में के.सी. डे के गाये जिन दो गीतों की चर्चा ऊपर की
पंक्तियों में की गई है, आइए आपको वही दोनों गीत सुनवाते हैं।
फिल्म धूप छाँव : “बाबा मन की आँखें खोल...” : के.सी. डे
फिल्म धूप छाँव : “तेरी गठरी में लागा चोर...” : के.सी. डे
इसी गीत के साथ आज हम ‘भूली-बिसरी यादें’ के इस अंक को यहीं विराम देते
हैं। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी, हमें अवश्य लिखिएगा। आपकी
प्रतिक्रिया, सुझाव और समालोचना से हम इस स्तम्भ को और भी सुरुचिपूर्ण रूप
प्रदान कर सकते हैं। ‘स्मृतियों के झरोखे से : भारतीय सिनेमा के सौ साल’ के
आगामी अंक में बारी है- ‘मैंने देखी पहली फिल्म’ स्तम्भ की। अगला गुरुवार
मास का चौथा गुरुवार होगा। इस दिन हम प्रस्तुत करेंगे एक बेहद रोचक
संस्मरण। यदि आपने ‘मैंने देखी पहली फिल्म’ प्रतियोगिता के लिए अभी तक अपना
संस्मरण नहीं भेजा है तो हमें तत्काल radioplaybackindia@live.com पर हमें मेल करें।
प्रस्तुति : कृष्णमोहन मिश्र
“मैंने देखी पहली फिल्म” : आपके लिए एक रोचक प्रतियोगिता
दोस्तों, भारतीय सिनेमा अपने उदगम के 100 वर्ष पूरा करने जा रहा है।
फ़िल्में हमारे जीवन में बेहद खास महत्त्व रखती हैं, शायद ही हम में से कोई
अपनी पहली देखी हुई फिल्म को भूल सकता है। वो पहली बार थियेटर जाना, वो
संगी-साथी, वो सुरीले लम्हें। आपकी इन्हीं सब यादों को हम समेटेगें एक
प्रतियोगिता के माध्यम से। 100 से 500 शब्दों में लिख भेजिए अपनी पहली देखी
फिल्म का अनुभव radioplaybackindia@live.com
पर। मेल के शीर्षक में लिखियेगा ‘मैंने देखी पहली फिल्म’। सर्वश्रेष्ठ तीन
आलेखों को 500 रूपए मूल्य की पुस्तकें पुरस्कारस्वरुप प्रदान की जायेगीं।
तो देर किस बात की, यादों की खिड़कियों को खोलिए, कीबोर्ड पर उँगलियाँ जमाइए
और लिख डालिए अपनी देखी हुई पहली फिल्म का दिलचस्प अनुभव। प्रतियोगिता में
आलेख भेजने की अन्तिम तिथि 31अक्टूबर, 2012 है।

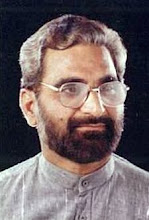
Comments