स्वरगोष्ठी – ८४ में आज
‘चतुर्भुज झूलत श्याम हिंडोला...’ : मल्हार अंग के कुछ अप्रचलित राग
‘चतुर्भुज झूलत श्याम हिंडोला...’ : मल्हार अंग के कुछ अप्रचलित राग
वर्षा ऋतु के संगीत पर केन्द्रित ‘स्वरगोष्ठी’ की यह श्रृंखला विगत सात सप्ताह से जारी है। परन्तु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब इस ऋतु ने भी विराम लेने का मन बना लिया है। अतः हम भी इस श्रृंखला को आज के अंक से विराम देने जा रहे हैं। पिछले अंकों में आपने मल्हार अंग के विविध रागों और वर्षा ऋतु की मनभावन कजरी गीतों का रसास्वादन किया था। आज इस श्रृंखला के समापन अंक में मल्हार अंग के कुछ अप्रचलित रागों पर चर्चा करेंगे और संगीत-जगत के कुछ शीर्षस्थ कलासाधकों से इन रागों में निबद्ध रचनाओं का रसास्वादन भी करेंगे।
 |
| पण्डित सवाई गन्धर्व |
मल्हार अंग का एक मधुर राग है- नट मल्हार। आजकल यह राग बहुत कम सुनाई देता है। यह राग नट और मल्हार अंग के मेल से बना है। इसे विलावल थाट का राग माना जाता है। इस राग में दोनों निषाद का प्रयोग होता है, शेष सभी स्वर शुद्ध प्रयुक्त होते हैं। इसका वादी मध्यम और संवादी षडज होता है। इसराज और मयूर वीणा-वादक पं. श्रीकुमार मिश्र के अनुसार इस राग के गायन-वादन में नट अंग की स्वर-संगति, सा रे s रे ग s ग म रे... मियाँ की मल्हार की, म रे प नि(कोमल) ध नि सां ध नि(कोमल) म प... तथा गौड़ मल्हार की स्वर संगति, म प ध नि सां s ध प म... की जाती है। इस राग के माध्यम से नायिका की विकल मनःस्थिति का सम्प्रेषण भावपूर्ण ढंग से की जा सकती है। प्रायः मध्य लय की रचनाएँ इस राग में बड़ी भली लगती है।
आइए अब आपको राग नट मल्हार की एक दुर्लभ रिकार्डिंग सुनवाते है। इसे बीसवीं शताब्दी के आरम्भिक दशकों के सुविख्यात विद्वान पण्डित सवाई गन्धर्व अर्थात पण्डित रामचन्द्र गणेश कुण्डगोलकर ने स्वर दिया है। पण्डित गन्धर्व किराना घराना के संवाहक उस्ताद अब्दुल करीम खाँ के शिष्य और पण्डित भीमसेन जोशी, विदुषी गंगुबाई हंगल, पण्डित फिरोज दस्तूर, पण्डित वासवराज राजगुरु आदि महान संगीतज्ञों के गुरु थे। राग नट मल्हार की मध्य लय, तीनताल में यह मोहक रचना आप भी सुनिए।
राग नट मल्हार : ‘बनरा बन आया...’ : पण्डित सवाई गन्धर्व
मल्हार का ही एक प्रकार है, राग जयन्त या जयन्ती मल्हार। इसके नाम से आभास हो जाता है कि यह राग
 |
| पण्डित विनायकराव पटवर्धन |
आपको सुनवाने के लिए हमने राग जयन्त मल्हार की एक प्राचीन किन्तु मोहक बन्दिश का चयन किया है। अपने समय के बहुआयामी संगीतज्ञ पण्डित विनायकराव पटवर्धन ने इस रचना को स्वर दिया है। पण्डित पटवर्धन ने न केवल रागदारी संगीत के क्षेत्र में, बल्कि सवाक फिल्मों के प्रारम्भिक दौर में भी अपना अनमोल योगदान किया था। लीजिए, राग जयन्त मल्हार की तीनताल में निबद्ध यह रचना आप भी सुनिए।
राग जयन्त मल्हार : ‘ऋतु आई सावन की...’ : पण्डित विनायकराव पटवर्धन
 राग जयन्त मल्हार का उपयोग फिल्म-संगीत में एकमात्र संगीतकार बसन्त देसाई ने ही किया था। उन्हें मल्हार अंग के राग अत्यन्त प्रिय थे। उनके द्वारा स्वरबद्ध गीतों की सूची में मल्हार की विविधता के स्पष्ट दर्शन होते हैं। १९७५ में बसन्त देसाई की संगीतबद्ध फिल्म ‘शक’ प्रदर्शित हुई थी। यह उनकी संगीतबद्ध अन्तिम फिल्म थी। फिल्म के प्रदर्शन से पहले ही एक लिफ्ट दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। फिल्म ‘शक’ में श्री देसाई ने गुलजार के लिखे एक गीत- ‘मेहा बरसने लगा है...’ को राग जयन्त मल्हार के स्वरों में ढाल कर कर्णप्रिय रूप दिया है। आशा भोसले के स्वरों में आप भी यह गीत सुनिए-
राग जयन्त मल्हार का उपयोग फिल्म-संगीत में एकमात्र संगीतकार बसन्त देसाई ने ही किया था। उन्हें मल्हार अंग के राग अत्यन्त प्रिय थे। उनके द्वारा स्वरबद्ध गीतों की सूची में मल्हार की विविधता के स्पष्ट दर्शन होते हैं। १९७५ में बसन्त देसाई की संगीतबद्ध फिल्म ‘शक’ प्रदर्शित हुई थी। यह उनकी संगीतबद्ध अन्तिम फिल्म थी। फिल्म के प्रदर्शन से पहले ही एक लिफ्ट दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। फिल्म ‘शक’ में श्री देसाई ने गुलजार के लिखे एक गीत- ‘मेहा बरसने लगा है...’ को राग जयन्त मल्हार के स्वरों में ढाल कर कर्णप्रिय रूप दिया है। आशा भोसले के स्वरों में आप भी यह गीत सुनिए-
फिल्म शक : ‘मेहा बरसने लगा है आज की रात...’ : संगीत – बसन्त देसाई
 |
| पं. भीमसेन जोशी |
राग छाया मल्हार : ‘सखी श्याम नहीं आए...’ : पण्डित भीमसेन जोशी
 |
| पण्डित जसराज |
राग चरजू की मल्हार : ‘चतुर्भुज झूलत श्याम हिंडोला...’ : पण्डित जसराज
 और अब अन्त में हम आपको १९७९ में प्रदर्शित फिल्म ‘मीरा’ का एक गीत सुनवाते हैं। गीतकार गुलजार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में भक्त कवयित्री मीराबाई का जीवन-दर्शन रेखांकित किया गया था। मीराबाई की जीवनगाथा में उन्हीं के पदों को विश्वविख्यात सितार-वादक पण्डित रविशंकर ने संगीतबद्ध किया था। मीरा के इन पदों में एक पद है- ‘बादल देख डरी मैं...’, जिसे पण्डित रविशंकर ने राग मीराबाई की मल्हार में स्वरबद्ध किया है और इसे स्वर दिया है, गायिका वाणी जयराम ने।
और अब अन्त में हम आपको १९७९ में प्रदर्शित फिल्म ‘मीरा’ का एक गीत सुनवाते हैं। गीतकार गुलजार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में भक्त कवयित्री मीराबाई का जीवन-दर्शन रेखांकित किया गया था। मीराबाई की जीवनगाथा में उन्हीं के पदों को विश्वविख्यात सितार-वादक पण्डित रविशंकर ने संगीतबद्ध किया था। मीरा के इन पदों में एक पद है- ‘बादल देख डरी मैं...’, जिसे पण्डित रविशंकर ने राग मीराबाई की मल्हार में स्वरबद्ध किया है और इसे स्वर दिया है, गायिका वाणी जयराम ने।
राग मीराबाई की मल्हार : ‘बादल देख डरी हो श्याम...’ : वाणी जयराम
फिल्म ‘मीरा’ के इस गीत की रिकार्डिंग सुप्रसिद्ध लेखिका और रेडियो प्लेबैक इण्डिया की शुभचिन्तक श्रीमती इन्दु पुरी गोस्वामी ने भेजी थी। उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अब हम आज के इस अंक को यहीं विराम देते हैं।
आज की पहेली
आज की ‘संगीत-पहेली’ में हम आपको एक सुविख्यात वादक कलाकार की आवाज़ में गायन का एक अंश सुनवा रहे हैं। इसे सुन कर आपको दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ९०वें अंक तक जिस प्रतिभागी के सर्वाधिक अंक होंगे, उन्हें इस श्रृंखला का विजेता घोषित किया जाएगा।
१_ संगीत के इस अंश में गायन स्वर किस विख्यात भारतीय वादक कलाकार का है?
२_ संगीत का यह अंश किस राग की ओर संकेत करता है?
२_ संगीत का यह अंश किस राग की ओर संकेत करता है?
आप अपने उत्तर केवल swargoshthi@gmail.com पर ही शनिवार मध्यरात्रि तक भेजें। comments में दिये गए उत्तर मान्य नहीं होंगे। विजेता का नाम हम ‘स्वरगोष्ठी’ के ८६वें अंक में प्रकाशित करेंगे। इस अंक में प्रस्तुत गीत-संगीत, राग, अथवा कलासाधक के बारे में यदि आप कोई जानकारी या अपने किसी अनुभव को हम सबके बीच बाँटना चाहते हैं तो हम आपका इस संगोष्ठी में स्वागत करते हैं। आप पृष्ठ के नीचे दिये गए comments के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। हमसे सीधे सम्पर्क के लिए swargoshthi@gmail.com पर अपना सन्देश भेज सकते हैं।
पिछली पहेली के विजेता
‘स्वरगोष्ठी’ के ८२वें अंक की पहेली में हमने आपको एक बेहद लोकप्रिय कजरी गीत का अंतरा सुनवा कर आपसे दो प्रश्न पूछे थे। पहले प्रश्न का सही उत्तर है- “कैसे खेले जइबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरि आइल ननदी...” और दूसरे का सही उत्तर है- ताल कहरवा। दोनों प्रश्नों के सही उत्तर लखनऊ के प्रकाश गोविन्द, जबलपुर की क्षिति तिवारी और मीरजापुर (उ.प्र.) के डॉ. पी.के. त्रिपाठी ने दिया है। इन्हें मिलते हैं २-२ अंक। तीनों प्रतिभागियों को रेडियो प्लेबैक इण्डिया की ओर से हार्दिक बधाई।
झरोखा अगले अंक का
मित्रों, ‘स्वरगोष्ठी’ के आज के अंक में हमने वर्षा ऋतु के प्रचलित गीत, संगीत और रागों की श्रृंखला को विराम दिया है। अगले अंक में तंत्र वाद्य के राष्ट्रीय ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त कलासाधक का स्मरण करेंगे। आगामी २८ अगस्त को इनकी जयन्ती भी मनाई जाएगी। इस अवसर पर हम उन्हें स्मरण करेंगे और भावभीनी संगीतांजलि अर्पित करेंगे। अगले रविवार को प्रातः ९-३० पर आयोजित अपनी इस गोष्ठी में आप हमारे सहभागी बनिए। हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी।
कृष्णमोहन मिश्र

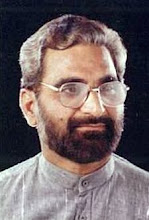
Comments