स्वरगोष्ठी – ७३ में आज
जिनके वाद्यवृन्द का सारा विश्व दीवाना हुआ
भारतीय पारसी परिवार में एक समर्पित वायलिन-वादक के घर जन्में जुबीन मेहता को उनके पिता ने किशोरावस्था में जब संगीत शिक्षा के लिए पुणे भेजा तो उनका मन क्रिकेट खेलने में अधिक लगता था। अपने पुत्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए पिता ने एक और प्रयास किया। इस बार जुबीन को सेण्ट ज़ेवियर कालेज में प्रवेश दिलाया गया, ताकि बेटा चिकित्सक बन सके। परन्तु पढ़ाई अधूरी छोड़कर वे संगीत के क्षेत्र में पुनः वापस लौट आए।
 ‘स्वरगोष्ठी’ के एक नए अंक के साथ मैं, कृष्णमोहन मिश्र, आपकी गोष्ठी में पुनः उपस्थित हूँ और आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के अंक में पाश्चात्य संगीत के एक ऐसे भारतीय कलासाधक की चर्चा करेंगे, जिसके संगीत कार्यक्रमों ने कई दशकों से पूरे विश्व को दीवाना बना रखा है। जुबीन मेहता का जन्म २९ अप्रैल, १९३६ को तत्कालीन बम्बई के एक पारसी परिवार में हुआ था। जुबीन की माँ का नाम तेहमिना और पिता का नाम मेहली मेहता है। मेहली मेहता एक समर्पित संगीत-सेवी थे, जिन्होने अपने परिवार को एक चुनौती सी देते हुए वायलिन-वादक बनाना पसन्द किया। जुबीन के पिता मेहली मेहता ने ही भारत के प्रथम वाद्य-वृन्द-दल ‘बम्बई सिम्फनी’ की स्थापना की थी। संगीत के ऐसे ही परिवेश में जुबीन बड़े हुए। अपने पिता की धुनें उन्हें हमेशा घेरे रहती थी। मात्र तेरह वर्ष की आयु में ही पिता ने जुबीन के ऊपर ‘बम्बई सिम्फनी’ में सहायक प्रबन्धक का दायित्व सौंप दिया। इस आयु में भी उनकी सांगीतिक प्रतिभा अत्यन्त मुखर थी। यद्यपि परिपक्व संगीतकार बनने तक जुबीन का मन कई बार डावाडोल हुआ, अन्ततः उन्होने पाश्चात्य संगीत का वह शिखर स्पर्श कर लिया जहाँ पहुँच कर हर कलाकार को पूरी ‘वसुधा’ एक ‘कुटुम्ब’ के रूप में परिलक्षित होने लगती है। जुबीन मेहता के जीवन के कुछ रोचक प्रसंगों पर चर्चा हम जारी रखेंगे, उससे पहले आप उनकी एक संगीत-रचना सुनिए। वर्ष २००७ में जुबीन मेहता ने विएना में नव-वर्ष के अवसर पर वाद्य-वृन्द की यह रचना प्रस्तुत की थी।
‘स्वरगोष्ठी’ के एक नए अंक के साथ मैं, कृष्णमोहन मिश्र, आपकी गोष्ठी में पुनः उपस्थित हूँ और आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के अंक में पाश्चात्य संगीत के एक ऐसे भारतीय कलासाधक की चर्चा करेंगे, जिसके संगीत कार्यक्रमों ने कई दशकों से पूरे विश्व को दीवाना बना रखा है। जुबीन मेहता का जन्म २९ अप्रैल, १९३६ को तत्कालीन बम्बई के एक पारसी परिवार में हुआ था। जुबीन की माँ का नाम तेहमिना और पिता का नाम मेहली मेहता है। मेहली मेहता एक समर्पित संगीत-सेवी थे, जिन्होने अपने परिवार को एक चुनौती सी देते हुए वायलिन-वादक बनाना पसन्द किया। जुबीन के पिता मेहली मेहता ने ही भारत के प्रथम वाद्य-वृन्द-दल ‘बम्बई सिम्फनी’ की स्थापना की थी। संगीत के ऐसे ही परिवेश में जुबीन बड़े हुए। अपने पिता की धुनें उन्हें हमेशा घेरे रहती थी। मात्र तेरह वर्ष की आयु में ही पिता ने जुबीन के ऊपर ‘बम्बई सिम्फनी’ में सहायक प्रबन्धक का दायित्व सौंप दिया। इस आयु में भी उनकी सांगीतिक प्रतिभा अत्यन्त मुखर थी। यद्यपि परिपक्व संगीतकार बनने तक जुबीन का मन कई बार डावाडोल हुआ, अन्ततः उन्होने पाश्चात्य संगीत का वह शिखर स्पर्श कर लिया जहाँ पहुँच कर हर कलाकार को पूरी ‘वसुधा’ एक ‘कुटुम्ब’ के रूप में परिलक्षित होने लगती है। जुबीन मेहता के जीवन के कुछ रोचक प्रसंगों पर चर्चा हम जारी रखेंगे, उससे पहले आप उनकी एक संगीत-रचना सुनिए। वर्ष २००७ में जुबीन मेहता ने विएना में नव-वर्ष के अवसर पर वाद्य-वृन्द की यह रचना प्रस्तुत की थी।
जुबीन मेहता : वियेना-२००७ : नव-वर्ष कन्सर्ट
जुबीन को उनके पिता ने पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा के लिए तत्कालीन विद्वान ओडेनी सेविनी के पास पुणे भेजा, किन्तु पुणे पहुँच कर उन्हें संगीत के स्थान पर क्रिकेट से कुछ अधिक लगाव हो गया। मेहली मेहता को यह जान कर कुछ निराशा हुई और उन्होने अपने पुत्र को चिकित्सा की पढ़ाई के लिए दाखिला दिलवा दिया। वर्ष १९५२ में एक ऐसी घटना घटी कि अपनी चिकित्सा की पढ़ाई छोड़ कर वापस संगीत के क्षेत्र में वापस लौट आए। दरअसल इसी वर्ष सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ यहूदी मेनहिन, भारत में अकाल-पीड़ितों के लिए धन-संग्रह के उद्देश्य से कंसर्ट करना चाहते थे। उन्होने भारत आकर जुबीन के पिता के वाद्य-वृन्द (आर्केस्ट्रा) ‘बम्बई सिम्फनी’ से इस नेक कार्य के लिए सहयोग माँगा। मेहली मेहता ने यहूदी मेनहिन को पूरा सहयोग दिया। एक पूर्वाभ्यास में जुबीन भी उपस्थित थे। पिता ने उस पूर्वाभ्यास में आर्केस्ट्रा संचालन में सहयोग के लिए जुबीन को संकेत किया। यहूदी मेनहिन उस नवयुवक का संचालन देख कर मुग्ध हो गए। जुबीन भी यहूदी मेनहिन के संगीत-ज्ञान से प्रभावित हुए और अपनी चिकित्सा की पढ़ाई छोड़ कर वापस संगीत-क्षेत्र में लौट आए। आइए, अब हम जुबीन मेहता की एक और रचना का आनन्द लेते हैं। ‘बीथोवेन सिम्फ़नी-६’ शीर्षक की यह रचना इसरायल फिलहार्मोनिका द्वारा जुबीन मेहता के निर्देशन में १० नवम्बर, २०१० को प्रस्तुत किया गया था।
जुबीन मेहता : ‘बीथोवेन सिम्फ़नी-६’ : इसरायल फिलहार्मोनिका
यहूदी मेनहिन से प्रेरणा और प्रोत्साहन पाकर जुबीन संगीत के क्षेत्र में वापस तो आ गए किन्तु उन्हें अपना संगीत-ज्ञान अधूरा लगा। संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होने वियना की म्यूजिक एकेडमी में प्रवेश ले लिया। उस दौरान जुबीन आर्थिक कठिनाइयों से जूझते रहे, किन्तु उनके सामने तो उज्ज्वल भविष्य बाँहें पसारे खड़ा था। एकेडमी के पहले ग्रीष्मावकाश में रिकार्ड की जाने वाली संगीत रचना में जुबीन को पहला अवसर एक वादक के रूप में मिला। इसके बाद तो सफलता उनके कदम चूमने लगी। वाद्य-वृन्द-संचालक के रूप में उन्हें जो सफलता मिली उसके लिए वे अपने प्रोफेसर हान्स स्वरास्की को श्रेय देते हैं। जुबीन मेहता १९६२ से १९६७ तक एक साथ दो वाद्य-वृन्द-दल, 'मॉण्ट्रियल सिम्फनी' तथा 'लॉस एंजिल्स फिलहार्मोनिक' के संचालक रहे। इसके अलावा १९७८ से १९९१ तक 'न्यूयार्क फिलहार्मोनिक' तथा 'इजराइल फिलहार्मोनिक' के संचालक भी रहे। २७ नवम्बर, १९९४ को इन्दिरा गाँधी स्टेडियम में इन्होंने इजराइल फिलहार्मोनिक का संचालन कर उपस्थित श्रोताओं का मन मोह लिया था। 'ए कंसर्ट फॉर पीस' के तहत आयोजित यह कार्यक्रम महात्मा गाँधी की १२५वीं जयन्ती पर उनकी स्मृति में समर्पित किया गया था। जुबीन मेहता को १९६६ में पद्मभूषण और २००१ में पद्मविभूषण से सम्मानित किया गया।
पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त संगीतज्ञ जुबीन मेहता भारतीय संगीत के प्रबल समर्थक हैं। सितारवादक पण्डित रविशंकर, जुबीन मेहता के प्रिय संगीतज्ञ हैं। जुबीन मेहता की कई वाद्य-वृन्द रचनाओं में रविशंकर जी का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। जुबीन मेहता के संचालन में लन्दन फिलहार्मोनिक आर्केस्ट्रा के साथ पण्डित रविशंकर ने एक बेहद आकर्षक रचना तैयार की थी, जिसे अब हम आपको सुनवा रहे हैं। इस रचना में मुख्य रूप से राग मियाँ की मल्हार के साथ अन्य कई रागों की एक माला का प्रयोग किया गया है। वर्षा ऋतु के परिवेश का साक्षात अनुभव करने के लिए आप यह रचना सुनें और मुझे आज के इस अंक से विराम लेने के लिए अनुमति दीजिए।
जुबीन मेहता - पण्डित रविशंकर : मियाँ की मल्हार और रागमाला : लन्दन फिलहार्मोनिक
आज की पहेली
आज की संगीत-पहेली में हम आपको सुनवा रहे हैं, किराना घराने के सुप्रसिद्ध गायक पण्डित फिरोज दस्तूर की आवाज़ में एक द्रुत खयाल की रचना। किशोरावस्था में सवाक फिल्मों के शुरुआती दौर की कुछ फिल्मों में उन्होने अपने स्वर का योगदान किया था। संगीत का यह अंश सुन कर आपको दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ८०वें अंक तक सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले पाठक/श्रोता हमारी तीसरी पहेली श्रृंखला के ‘विजेता’ होंगे।
१- संगीत के इस अंश को सुन राग पहचानिए और हमें राग का नाम बताइए।
२- उस्ताद अब्दुल करीम खाँ की परम्परा में गाने वाले और सवाई गन्धर्व के ही शिष्य एक सुविख्यात गायक थे, जो पण्डित फिरोज दस्तूर के गुरु-भाई थे, जिनका पिछले वर्ष जनवरी में निधन हुआ था। क्या आप दस्तूर जी के इन गुरु-भाई को पहचान रहे हैं? यदि हाँ तो हमें उस महान गायक का नाम बताइए।
आप अपने उत्तर हमें तत्काल swargoshthi@gmail.com पर भेजें। विजेता का नाम हम ‘स्वरगोष्ठी’ के ७५वें अंक में प्रकाशित करेंगे। इस अंक में प्रस्तुत गीत-संगीत, राग, अथवा कलासाधक के बारे में यदि आप कोई जानकारी या अपने किसी अनुभव को हम सबके बीच बाँटना चाहते हैं तो हम आपका इस संगोष्ठी में स्वागत करते हैं। आप पृष्ठ के नीचे दिये गए comments के माध्यम से अथवा swargoshthi@gmail.com पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं।
पिछली पहेली के विजेता
‘स्वरगोष्ठी’ के ७१वें अंक में हमने आपको १९५२ की फिल्म ‘बैजू बावरा’ से प्रसिद्ध जुगलबन्दी का एक अंश सुनवाया था। हमारे पहले प्रश्न का सही उत्तर है- उस्ताद अमीर खाँ और दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है- राग देशी। दोनों प्रश्नों के सही उत्तर मीरजापुर (उ.प्र.) के डॉ. पी.के. त्रिपाठी, जबलपुर की क्षिति तिवारी तथा पटना की अर्चना टण्डन ने दिया है। तीनों प्रतिभागियों को रेडियो प्लेबैक इण्डिया की ओर से हार्दिक बधाई।
मित्रों, पिछले सप्ताह से हमने आपकी प्रतिक्रियाओं, सन्देशों और सुझावों के लिए एक अलग साप्ताहिक स्तम्भ ‘आपकी बात’ आरम्भ किया है। अब प्रत्येक शुक्रवार को ‘रेडियो प्लेबैक इण्डिया’पर आपके भेजे सन्देश को हम अपने सजीव कार्यक्रम में शामिल किया करेंगे। आप हमें swargoshthi@gmail.com अथवा cine.paheli@yahoo.com के पते पर आज ही लिखें।
झरोखा अगले अंक का
मित्रों, आप जानते ही हैं कि इस वर्ष, हम भारत में फिल्म निर्माण का सौवाँ वर्ष मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में ‘स्वरगोष्ठी’ के अगले अंक में हम सवाक फिल्मों के प्रारम्भिक दौर के गायक-अभिनेता फिरोज दस्तूर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आपसे चर्चा करेंगे। आगामी रविवार को प्रातः ९-३० बजे आप और हम ‘स्वरगोष्ठी’ के अगले अंक में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हमें विराम लेने की अनुमति दीजिए।
कृष्णमोहन मिश्र
जिनके वाद्यवृन्द का सारा विश्व दीवाना हुआ
भारतीय पारसी परिवार में एक समर्पित वायलिन-वादक के घर जन्में जुबीन मेहता को उनके पिता ने किशोरावस्था में जब संगीत शिक्षा के लिए पुणे भेजा तो उनका मन क्रिकेट खेलने में अधिक लगता था। अपने पुत्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए पिता ने एक और प्रयास किया। इस बार जुबीन को सेण्ट ज़ेवियर कालेज में प्रवेश दिलाया गया, ताकि बेटा चिकित्सक बन सके। परन्तु पढ़ाई अधूरी छोड़कर वे संगीत के क्षेत्र में पुनः वापस लौट आए।
 ‘स्वरगोष्ठी’ के एक नए अंक के साथ मैं, कृष्णमोहन मिश्र, आपकी गोष्ठी में पुनः उपस्थित हूँ और आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के अंक में पाश्चात्य संगीत के एक ऐसे भारतीय कलासाधक की चर्चा करेंगे, जिसके संगीत कार्यक्रमों ने कई दशकों से पूरे विश्व को दीवाना बना रखा है। जुबीन मेहता का जन्म २९ अप्रैल, १९३६ को तत्कालीन बम्बई के एक पारसी परिवार में हुआ था। जुबीन की माँ का नाम तेहमिना और पिता का नाम मेहली मेहता है। मेहली मेहता एक समर्पित संगीत-सेवी थे, जिन्होने अपने परिवार को एक चुनौती सी देते हुए वायलिन-वादक बनाना पसन्द किया। जुबीन के पिता मेहली मेहता ने ही भारत के प्रथम वाद्य-वृन्द-दल ‘बम्बई सिम्फनी’ की स्थापना की थी। संगीत के ऐसे ही परिवेश में जुबीन बड़े हुए। अपने पिता की धुनें उन्हें हमेशा घेरे रहती थी। मात्र तेरह वर्ष की आयु में ही पिता ने जुबीन के ऊपर ‘बम्बई सिम्फनी’ में सहायक प्रबन्धक का दायित्व सौंप दिया। इस आयु में भी उनकी सांगीतिक प्रतिभा अत्यन्त मुखर थी। यद्यपि परिपक्व संगीतकार बनने तक जुबीन का मन कई बार डावाडोल हुआ, अन्ततः उन्होने पाश्चात्य संगीत का वह शिखर स्पर्श कर लिया जहाँ पहुँच कर हर कलाकार को पूरी ‘वसुधा’ एक ‘कुटुम्ब’ के रूप में परिलक्षित होने लगती है। जुबीन मेहता के जीवन के कुछ रोचक प्रसंगों पर चर्चा हम जारी रखेंगे, उससे पहले आप उनकी एक संगीत-रचना सुनिए। वर्ष २००७ में जुबीन मेहता ने विएना में नव-वर्ष के अवसर पर वाद्य-वृन्द की यह रचना प्रस्तुत की थी।
‘स्वरगोष्ठी’ के एक नए अंक के साथ मैं, कृष्णमोहन मिश्र, आपकी गोष्ठी में पुनः उपस्थित हूँ और आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के अंक में पाश्चात्य संगीत के एक ऐसे भारतीय कलासाधक की चर्चा करेंगे, जिसके संगीत कार्यक्रमों ने कई दशकों से पूरे विश्व को दीवाना बना रखा है। जुबीन मेहता का जन्म २९ अप्रैल, १९३६ को तत्कालीन बम्बई के एक पारसी परिवार में हुआ था। जुबीन की माँ का नाम तेहमिना और पिता का नाम मेहली मेहता है। मेहली मेहता एक समर्पित संगीत-सेवी थे, जिन्होने अपने परिवार को एक चुनौती सी देते हुए वायलिन-वादक बनाना पसन्द किया। जुबीन के पिता मेहली मेहता ने ही भारत के प्रथम वाद्य-वृन्द-दल ‘बम्बई सिम्फनी’ की स्थापना की थी। संगीत के ऐसे ही परिवेश में जुबीन बड़े हुए। अपने पिता की धुनें उन्हें हमेशा घेरे रहती थी। मात्र तेरह वर्ष की आयु में ही पिता ने जुबीन के ऊपर ‘बम्बई सिम्फनी’ में सहायक प्रबन्धक का दायित्व सौंप दिया। इस आयु में भी उनकी सांगीतिक प्रतिभा अत्यन्त मुखर थी। यद्यपि परिपक्व संगीतकार बनने तक जुबीन का मन कई बार डावाडोल हुआ, अन्ततः उन्होने पाश्चात्य संगीत का वह शिखर स्पर्श कर लिया जहाँ पहुँच कर हर कलाकार को पूरी ‘वसुधा’ एक ‘कुटुम्ब’ के रूप में परिलक्षित होने लगती है। जुबीन मेहता के जीवन के कुछ रोचक प्रसंगों पर चर्चा हम जारी रखेंगे, उससे पहले आप उनकी एक संगीत-रचना सुनिए। वर्ष २००७ में जुबीन मेहता ने विएना में नव-वर्ष के अवसर पर वाद्य-वृन्द की यह रचना प्रस्तुत की थी। जुबीन मेहता : वियेना-२००७ : नव-वर्ष कन्सर्ट
जुबीन को उनके पिता ने पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा के लिए तत्कालीन विद्वान ओडेनी सेविनी के पास पुणे भेजा, किन्तु पुणे पहुँच कर उन्हें संगीत के स्थान पर क्रिकेट से कुछ अधिक लगाव हो गया। मेहली मेहता को यह जान कर कुछ निराशा हुई और उन्होने अपने पुत्र को चिकित्सा की पढ़ाई के लिए दाखिला दिलवा दिया। वर्ष १९५२ में एक ऐसी घटना घटी कि अपनी चिकित्सा की पढ़ाई छोड़ कर वापस संगीत के क्षेत्र में वापस लौट आए। दरअसल इसी वर्ष सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ यहूदी मेनहिन, भारत में अकाल-पीड़ितों के लिए धन-संग्रह के उद्देश्य से कंसर्ट करना चाहते थे। उन्होने भारत आकर जुबीन के पिता के वाद्य-वृन्द (आर्केस्ट्रा) ‘बम्बई सिम्फनी’ से इस नेक कार्य के लिए सहयोग माँगा। मेहली मेहता ने यहूदी मेनहिन को पूरा सहयोग दिया। एक पूर्वाभ्यास में जुबीन भी उपस्थित थे। पिता ने उस पूर्वाभ्यास में आर्केस्ट्रा संचालन में सहयोग के लिए जुबीन को संकेत किया। यहूदी मेनहिन उस नवयुवक का संचालन देख कर मुग्ध हो गए। जुबीन भी यहूदी मेनहिन के संगीत-ज्ञान से प्रभावित हुए और अपनी चिकित्सा की पढ़ाई छोड़ कर वापस संगीत-क्षेत्र में लौट आए। आइए, अब हम जुबीन मेहता की एक और रचना का आनन्द लेते हैं। ‘बीथोवेन सिम्फ़नी-६’ शीर्षक की यह रचना इसरायल फिलहार्मोनिका द्वारा जुबीन मेहता के निर्देशन में १० नवम्बर, २०१० को प्रस्तुत किया गया था।
जुबीन मेहता : ‘बीथोवेन सिम्फ़नी-६’ : इसरायल फिलहार्मोनिका
यहूदी मेनहिन से प्रेरणा और प्रोत्साहन पाकर जुबीन संगीत के क्षेत्र में वापस तो आ गए किन्तु उन्हें अपना संगीत-ज्ञान अधूरा लगा। संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होने वियना की म्यूजिक एकेडमी में प्रवेश ले लिया। उस दौरान जुबीन आर्थिक कठिनाइयों से जूझते रहे, किन्तु उनके सामने तो उज्ज्वल भविष्य बाँहें पसारे खड़ा था। एकेडमी के पहले ग्रीष्मावकाश में रिकार्ड की जाने वाली संगीत रचना में जुबीन को पहला अवसर एक वादक के रूप में मिला। इसके बाद तो सफलता उनके कदम चूमने लगी। वाद्य-वृन्द-संचालक के रूप में उन्हें जो सफलता मिली उसके लिए वे अपने प्रोफेसर हान्स स्वरास्की को श्रेय देते हैं। जुबीन मेहता १९६२ से १९६७ तक एक साथ दो वाद्य-वृन्द-दल, 'मॉण्ट्रियल सिम्फनी' तथा 'लॉस एंजिल्स फिलहार्मोनिक' के संचालक रहे। इसके अलावा १९७८ से १९९१ तक 'न्यूयार्क फिलहार्मोनिक' तथा 'इजराइल फिलहार्मोनिक' के संचालक भी रहे। २७ नवम्बर, १९९४ को इन्दिरा गाँधी स्टेडियम में इन्होंने इजराइल फिलहार्मोनिक का संचालन कर उपस्थित श्रोताओं का मन मोह लिया था। 'ए कंसर्ट फॉर पीस' के तहत आयोजित यह कार्यक्रम महात्मा गाँधी की १२५वीं जयन्ती पर उनकी स्मृति में समर्पित किया गया था। जुबीन मेहता को १९६६ में पद्मभूषण और २००१ में पद्मविभूषण से सम्मानित किया गया।
पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त संगीतज्ञ जुबीन मेहता भारतीय संगीत के प्रबल समर्थक हैं। सितारवादक पण्डित रविशंकर, जुबीन मेहता के प्रिय संगीतज्ञ हैं। जुबीन मेहता की कई वाद्य-वृन्द रचनाओं में रविशंकर जी का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। जुबीन मेहता के संचालन में लन्दन फिलहार्मोनिक आर्केस्ट्रा के साथ पण्डित रविशंकर ने एक बेहद आकर्षक रचना तैयार की थी, जिसे अब हम आपको सुनवा रहे हैं। इस रचना में मुख्य रूप से राग मियाँ की मल्हार के साथ अन्य कई रागों की एक माला का प्रयोग किया गया है। वर्षा ऋतु के परिवेश का साक्षात अनुभव करने के लिए आप यह रचना सुनें और मुझे आज के इस अंक से विराम लेने के लिए अनुमति दीजिए।
जुबीन मेहता - पण्डित रविशंकर : मियाँ की मल्हार और रागमाला : लन्दन फिलहार्मोनिक
आज की पहेली
आज की संगीत-पहेली में हम आपको सुनवा रहे हैं, किराना घराने के सुप्रसिद्ध गायक पण्डित फिरोज दस्तूर की आवाज़ में एक द्रुत खयाल की रचना। किशोरावस्था में सवाक फिल्मों के शुरुआती दौर की कुछ फिल्मों में उन्होने अपने स्वर का योगदान किया था। संगीत का यह अंश सुन कर आपको दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ८०वें अंक तक सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले पाठक/श्रोता हमारी तीसरी पहेली श्रृंखला के ‘विजेता’ होंगे।
१- संगीत के इस अंश को सुन राग पहचानिए और हमें राग का नाम बताइए।
२- उस्ताद अब्दुल करीम खाँ की परम्परा में गाने वाले और सवाई गन्धर्व के ही शिष्य एक सुविख्यात गायक थे, जो पण्डित फिरोज दस्तूर के गुरु-भाई थे, जिनका पिछले वर्ष जनवरी में निधन हुआ था। क्या आप दस्तूर जी के इन गुरु-भाई को पहचान रहे हैं? यदि हाँ तो हमें उस महान गायक का नाम बताइए।
आप अपने उत्तर हमें तत्काल swargoshthi@gmail.com पर भेजें। विजेता का नाम हम ‘स्वरगोष्ठी’ के ७५वें अंक में प्रकाशित करेंगे। इस अंक में प्रस्तुत गीत-संगीत, राग, अथवा कलासाधक के बारे में यदि आप कोई जानकारी या अपने किसी अनुभव को हम सबके बीच बाँटना चाहते हैं तो हम आपका इस संगोष्ठी में स्वागत करते हैं। आप पृष्ठ के नीचे दिये गए comments के माध्यम से अथवा swargoshthi@gmail.com पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं।
पिछली पहेली के विजेता
‘स्वरगोष्ठी’ के ७१वें अंक में हमने आपको १९५२ की फिल्म ‘बैजू बावरा’ से प्रसिद्ध जुगलबन्दी का एक अंश सुनवाया था। हमारे पहले प्रश्न का सही उत्तर है- उस्ताद अमीर खाँ और दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है- राग देशी। दोनों प्रश्नों के सही उत्तर मीरजापुर (उ.प्र.) के डॉ. पी.के. त्रिपाठी, जबलपुर की क्षिति तिवारी तथा पटना की अर्चना टण्डन ने दिया है। तीनों प्रतिभागियों को रेडियो प्लेबैक इण्डिया की ओर से हार्दिक बधाई।
मित्रों, पिछले सप्ताह से हमने आपकी प्रतिक्रियाओं, सन्देशों और सुझावों के लिए एक अलग साप्ताहिक स्तम्भ ‘आपकी बात’ आरम्भ किया है। अब प्रत्येक शुक्रवार को ‘रेडियो प्लेबैक इण्डिया’पर आपके भेजे सन्देश को हम अपने सजीव कार्यक्रम में शामिल किया करेंगे। आप हमें swargoshthi@gmail.com अथवा cine.paheli@yahoo.com के पते पर आज ही लिखें।
झरोखा अगले अंक का
मित्रों, आप जानते ही हैं कि इस वर्ष, हम भारत में फिल्म निर्माण का सौवाँ वर्ष मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में ‘स्वरगोष्ठी’ के अगले अंक में हम सवाक फिल्मों के प्रारम्भिक दौर के गायक-अभिनेता फिरोज दस्तूर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आपसे चर्चा करेंगे। आगामी रविवार को प्रातः ९-३० बजे आप और हम ‘स्वरगोष्ठी’ के अगले अंक में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हमें विराम लेने की अनुमति दीजिए।
कृष्णमोहन मिश्र

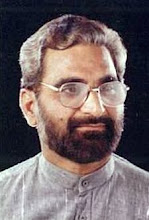
Comments
aabhaar !!