भारतीय सिनेमा के सौ साल – 37
कारवाँ सिने-संगीत का‘एक बार उन्हें मिला दे, फिर मेरी तौबा मौला...’
भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष में ‘रेडियो प्लेबैक इण्डिया’ द्वारा आयोजित
विशेष अनुष्ठान- ‘कारवाँ सिने-संगीत का’ में आप सभी सिनेमा-प्रेमियों का
हार्दिक स्वागत है। आज माह का चौथा गुरुवार है और माह के दूसरे और चौथे
गुरुवार को हम ‘कारवाँ सिने-संगीत का’ स्तम्भ के अन्तर्गत ‘रेडियो प्लेबैक
इण्डिया’ के संचालक मण्डल के सदस्य सुजॉय चटर्जी की प्रकाशित पुस्तक
‘कारवाँ सिने-संगीत का’ से किसी रोचक प्रसंग का उल्लेख करते हैं। आज के अंक
में हम भारतीय फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध पार्श्वगायक मोहम्मद रफी के
प्रारम्भिक दौर का ज़िक्र करेंगे।
 1944 में रफ़ी ने बम्बई का रुख़ किया जहाँ श्यामसुन्दर ने ही उन्हें ‘विलेज गर्ल’ (उर्फ़ ‘गाँव की गोरी’) में गाने का मौका दिया। पर यह फ़िल्म १९४५ में प्रदर्शित हुई। इससे पहले १९४४ में ‘पहले आप’ प्रदर्शित हो गई जिसमें नौशाद ने रफ़ी से कुछ गीत गवाए थे। नौशाद से रफ़ी को मिलवाने का श्रेय हमीद भाई को जाता है। उन्होंने ही लखनऊ जाकर नौशाद के पिता से मिल कर, उनसे एक सिफ़ारिशनामा लेकर रफ़ी को दे दिया कि बम्बई जाकर इसे नौशाद को दिखाए। बम्बई जाकर नौशाद से रफ़ी की पहली मुलाक़ात का वर्णन विविध भारती पर नौशाद के साक्षात्कार में मिलता है– “जब मोहम्मद रफ़ी मेरे पास आए, तब वर्ल्डवार ख़त्म हुआ चाहता था। मुझे साल याद नहीं। उस वक़्त फ़िल्म प्रोड्यूसर्स को कम से कम एक वार-प्रोपागण्डा फ़िल्म ज़रूर बनाना पड़ता था। रफ़ी साहब लखनऊ से मेरे पास मेरे वालिद साहब का एक सिफ़ारिशी ख़त लेकर आए। छोटा सा तम्बूरा हाथ में लिए खड़े थे मेरे सामने। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने संगीत सीखा है, तो बोले कि उस्ताद बरकत अली ख़ाँ से सीखा है, जो उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ाँ साहब के छोटे भाई थे। मैंने उनको कहा कि इस वक़्त मेरे पास कोई गीत नहीं है जो मैं उनसे गवा सकता हूँ, पर एक कोरस ज़रूर है जिसमें अगर वो चाहें तो कुछ लाइनें गा सकते हैं। और वह गाना था “हिन्दुस्तान के हम हैं हिन्दुस्तान हमारा, हिन्दू मुस्लिम दोनों की आँखों का तारा...”। रफ़ी साहब ने दो लाइने गायीं जिसके लिए उन्हें 10 रुपये दिए गए। शाम, दुर्रानी और कुछ अन्य गायकों ने भी कुछ कुछ लाइनें गायीं।” और इस तरह से मोहम्मद रफ़ी का गाया पहला हिन्दी फ़िल्मी गीत बाहर आया। पर रेकॉर्ड पर इस गीत को “समूह गीत” लिखा गया है। आइए, अब हम आपको वही गीत सुनवाते हैं। आप गीत सुनिए और इस गीत में रफी साहब की आवाज़ को पहचानिए।
1944 में रफ़ी ने बम्बई का रुख़ किया जहाँ श्यामसुन्दर ने ही उन्हें ‘विलेज गर्ल’ (उर्फ़ ‘गाँव की गोरी’) में गाने का मौका दिया। पर यह फ़िल्म १९४५ में प्रदर्शित हुई। इससे पहले १९४४ में ‘पहले आप’ प्रदर्शित हो गई जिसमें नौशाद ने रफ़ी से कुछ गीत गवाए थे। नौशाद से रफ़ी को मिलवाने का श्रेय हमीद भाई को जाता है। उन्होंने ही लखनऊ जाकर नौशाद के पिता से मिल कर, उनसे एक सिफ़ारिशनामा लेकर रफ़ी को दे दिया कि बम्बई जाकर इसे नौशाद को दिखाए। बम्बई जाकर नौशाद से रफ़ी की पहली मुलाक़ात का वर्णन विविध भारती पर नौशाद के साक्षात्कार में मिलता है– “जब मोहम्मद रफ़ी मेरे पास आए, तब वर्ल्डवार ख़त्म हुआ चाहता था। मुझे साल याद नहीं। उस वक़्त फ़िल्म प्रोड्यूसर्स को कम से कम एक वार-प्रोपागण्डा फ़िल्म ज़रूर बनाना पड़ता था। रफ़ी साहब लखनऊ से मेरे पास मेरे वालिद साहब का एक सिफ़ारिशी ख़त लेकर आए। छोटा सा तम्बूरा हाथ में लिए खड़े थे मेरे सामने। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने संगीत सीखा है, तो बोले कि उस्ताद बरकत अली ख़ाँ से सीखा है, जो उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ाँ साहब के छोटे भाई थे। मैंने उनको कहा कि इस वक़्त मेरे पास कोई गीत नहीं है जो मैं उनसे गवा सकता हूँ, पर एक कोरस ज़रूर है जिसमें अगर वो चाहें तो कुछ लाइनें गा सकते हैं। और वह गाना था “हिन्दुस्तान के हम हैं हिन्दुस्तान हमारा, हिन्दू मुस्लिम दोनों की आँखों का तारा...”। रफ़ी साहब ने दो लाइने गायीं जिसके लिए उन्हें 10 रुपये दिए गए। शाम, दुर्रानी और कुछ अन्य गायकों ने भी कुछ कुछ लाइनें गायीं।” और इस तरह से मोहम्मद रफ़ी का गाया पहला हिन्दी फ़िल्मी गीत बाहर आया। पर रेकॉर्ड पर इस गीत को “समूह गीत” लिखा गया है। आइए, अब हम आपको वही गीत सुनवाते हैं। आप गीत सुनिए और इस गीत में रफी साहब की आवाज़ को पहचानिए।
फिल्म पहले आप : ‘हिन्दुस्तान के हम हैं हिन्दुस्तान हमारा...’ : मोहम्मद रफी और साथी
यह गीत न केवल रफ़ी साहब के करियर का एक महत्वपूर्ण गीत बना, बल्कि इसके गीतकार डी.एन. मधोक के लिए भी यह उतना ही महत्वपूर्ण गीत बना क्योंकि इस गीत में उनके धर्मनिरपेक्षता के शब्दों के प्रयोग के लिए उन्हें “महाकवि” के शीर्षक से सम्मानित किया गया था। ब्रिटिश राज ने इस गीत का मार्च-पास्ट गीत के रूप में विश्वयुद्ध में इस्तेमाल किया। भले ही “हिन्दुस्तान के हम हैं...” गीत के लिए रफ़ी का नाम रेकॉर्ड पर नहीं छपा, पर इसी फ़िल्म में नौशाद ने उनसे दो और गीत भी गवाए, जो शाम के साथ गाए हुए युगल गीत थे– “तुम दिल्ली मैं आगरे, मेरे दिल से निकले हाय...” और “एक बार उन्हें मिला दे, फिर मेरी तौबा मौला...”। एक गीत ज़ोहराबाई के साथ भी उनका गाया हुआ बताया जाता है “मोरे सैंयाजी ने भेजी चुंदरी”, पर रेकॉर्ड पर ‘ज़ोहराबाई और साथी’ बताया गया है। जो भी है, ‘पहले आप’ से नौशाद और रफ़ी की जो जोड़ी बनी थी, वह अन्त तक क़ायम रही। यहाँ थोड़ा रुक कर आइए, रफी के शुरुआती दौर के इन दोनों गीतों को सुनते हैं।
फिल्म पहले आप : “तुम दिल्ली मैं आगरे, मेरे दिल से निकले हाय...” : रफी और शाम
फिल्म पहले आप : “एक बार उन्हें मिला दे, फिर मेरी तौबा मौला...” : रफी और शाम
 1980 में रफ़ी साहब की अचानक मृत्यु के बाद नौशाद साहब ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विविध भारती के एक विशेष प्रसारण में कहा था – “यूँ तो सभी आते हैं दुनिया में मरने के लिए, मौत उसकी होती है जिसका दुनिया करे अफ़सोस। मीर तक़ी ‘मीर’ का यह शे’र मोहम्मद रफ़ी पर हर बहर सटीक बैठता है। वाक़ई मोहम्मद रफ़ी साहब ऐसे इन्सान, ऐसे कलाकार थे, जो फलक की बरसों की इबादत के बाद ही पैदा होते हैं। हिन्दुस्तान तो क्या, दुनिया के करोड़ों इन्सानों के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। रफ़ी की आवाज़ से लोगों का दिन शुरु होता था, और उनकी आवाज़ ही पर रात ढलती थी। मेरा उनका साथ बहुत पुराना था। आप सब जानते हैं, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा हादसा, ऐसा नुकसान मेरे लिए हुआ, आप सब के लिए हुआ, बल्कि मैं समझता हूँ कि संगीत के सात सुरों में से एक सुर कम हो गया है, छह सुर रह गए हैं।
1980 में रफ़ी साहब की अचानक मृत्यु के बाद नौशाद साहब ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विविध भारती के एक विशेष प्रसारण में कहा था – “यूँ तो सभी आते हैं दुनिया में मरने के लिए, मौत उसकी होती है जिसका दुनिया करे अफ़सोस। मीर तक़ी ‘मीर’ का यह शे’र मोहम्मद रफ़ी पर हर बहर सटीक बैठता है। वाक़ई मोहम्मद रफ़ी साहब ऐसे इन्सान, ऐसे कलाकार थे, जो फलक की बरसों की इबादत के बाद ही पैदा होते हैं। हिन्दुस्तान तो क्या, दुनिया के करोड़ों इन्सानों के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। रफ़ी की आवाज़ से लोगों का दिन शुरु होता था, और उनकी आवाज़ ही पर रात ढलती थी। मेरा उनका साथ बहुत पुराना था। आप सब जानते हैं, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा हादसा, ऐसा नुकसान मेरे लिए हुआ, आप सब के लिए हुआ, बल्कि मैं समझता हूँ कि संगीत के सात सुरों में से एक सुर कम हो गया है, छह सुर रह गए हैं।
गायकी तेरा हुस्न-ए-फ़न रफ़ी, तेरे फ़न पर हम सभी को नाज़ है,
ये सबक सीखा तेरे नग़मात से, ज़िंदगानी प्यार का एक साज़ है,
मेरी सरगम में भी तेरा ज़िक्र है, मेरे गीतों में तेरी आवाज़ है।
कहता है कोई दिल चला गया, दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समन्दर चला गया,
लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसिक़ी का पयम्बर चला गया।
तुझे नग़मों की जान अहले नज़र यूंही नहीं कहते, तेरे गीतों को दिल का हमसफ़र यूंही नहीं कहते,
सुनी सब ने मोहब्बत जवान आवाज़ में तेरी, धड़कता है हिन्दुस्तान आवाज़ में तेरी।”
ख़लीक अमरोहवी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने रफ़ी साहब पर काफ़ी शोध कार्य किया है। विविध भारती के एक कार्यक्रम में उन्होंने रफ़ी साहब से सम्बन्धित कई जानकारियाँ दी थीं जिनमें से कुछ यहाँ प्रस्तुत है। 24 दिसम्बर 1924 को कोटला सुल्तानपुर, पंजाब में जन्मे रफ़ी छह भाइयों में दूसरे नम्बर पर थे। उनके बाक़ी पाँच भाइयों के नाम हैं शफ़ी, इमरान, दीन, इस्माइल और सिद्दिक़। उनके बचपन में उनके मोहल्ले में एक फ़कीर आया करता था, गाता हुआ। रफ़ी उसकी आवाज़ से आकृष्ट होकर उसके पीछे चल पड़ता और बहुत दूर निकल जाया करता। उनके बड़े भाई के दोस्त हमीद ने पहली बार उनकी गायन प्रतिभा को महसूस किया और उन्हें इस तरफ़ प्रोत्साहित किया। रफ़ी उस्ताद बरकत अली ख़ाँ के सम्पर्क में आए और उनसे शास्त्रीय संगीत सीखना शुरु किया। उस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। हमीद के ही सहयोग से उन्हें लाहौर रेडियो में गाने का अवसर मिला। एक बार यूं हुआ कि कुंदनलाल सहगल लाहौर गए किसी शो के लिए। पर बिजली फ़ेल हो जाने की वजह से जब शो बाधित हुआ, तब आयोजकों ने शोर मचाती जनता के सामने रफ़ी को खड़ा कर दिया गाने के लिए। इतनी कम उम्र में शास्त्रीय संगीत की बारीक़ियों को देख सहगल भी चकित रह गए और उनकी तारीफ़ की। यह रफ़ी के करियर की पहली उपलब्धि रही। हमीद ने फिर उन्हें दिल्ली भेजा दिल्ली रेडियो में गाने के लिए। वहाँ फ़िरोज़ निज़ामी थे जिन्होंने रफ़ी को कई ज़रूरी बातें सिखाईं। आइए, अब हम आपको रफी साहब का गाया, फिल्म ‘विलेज गर्ल उर्फ गाँव की गोरी’ का वह पहला गीत, जो संगीतकार श्यामसुन्दर ने गवाया था, किन्तु यह फिल्म 1945 में प्रदर्शित हुई। इससे पहले 1944 में फिल्म ‘पहले आप’ प्रदर्शित हो चुकी थी।
फिल्म विलेज गर्ल उर्फ गाँव की गोरी : “दिल हो काबू में तो दिलदार की...” : रफी और साथी
‘रेडियो प्लेबैक इण्डिया’ के स्तम्भ ‘कारवाँ सिने-संगीत का’ के अन्तर्गत आज
हमने सुजॉय चटर्जी की इसी शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक के कुछ पृष्ठ उद्धरित
किये हैं। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी, हमें अवश्य लिखिएगा। आपकी
प्रतिक्रिया, सुझाव और समालोचना से हम इस स्तम्भ को और भी सुरुचिपूर्ण रूप
प्रदान कर सकते हैं। ‘कारवाँ सिने-संगीत का’ के आगामी अंक में आपके लिए हम
इस पुस्तक के कुछ और रोचक पृष्ठ लेकर उपस्थित होंगे। सुजॉय चटर्जी की
पुस्तक ‘कारवाँ सिने-संगीत का’ प्राप्त करने के लिए तथा अपनी प्रतिक्रिया
और सुझाव हमें भेजने के लिए radioplaybackindia@live.com पर अपना सन्देश भेजें।
प्रस्तुति : कृष्णमोहन मिश्र

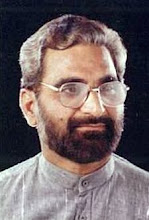

Comments